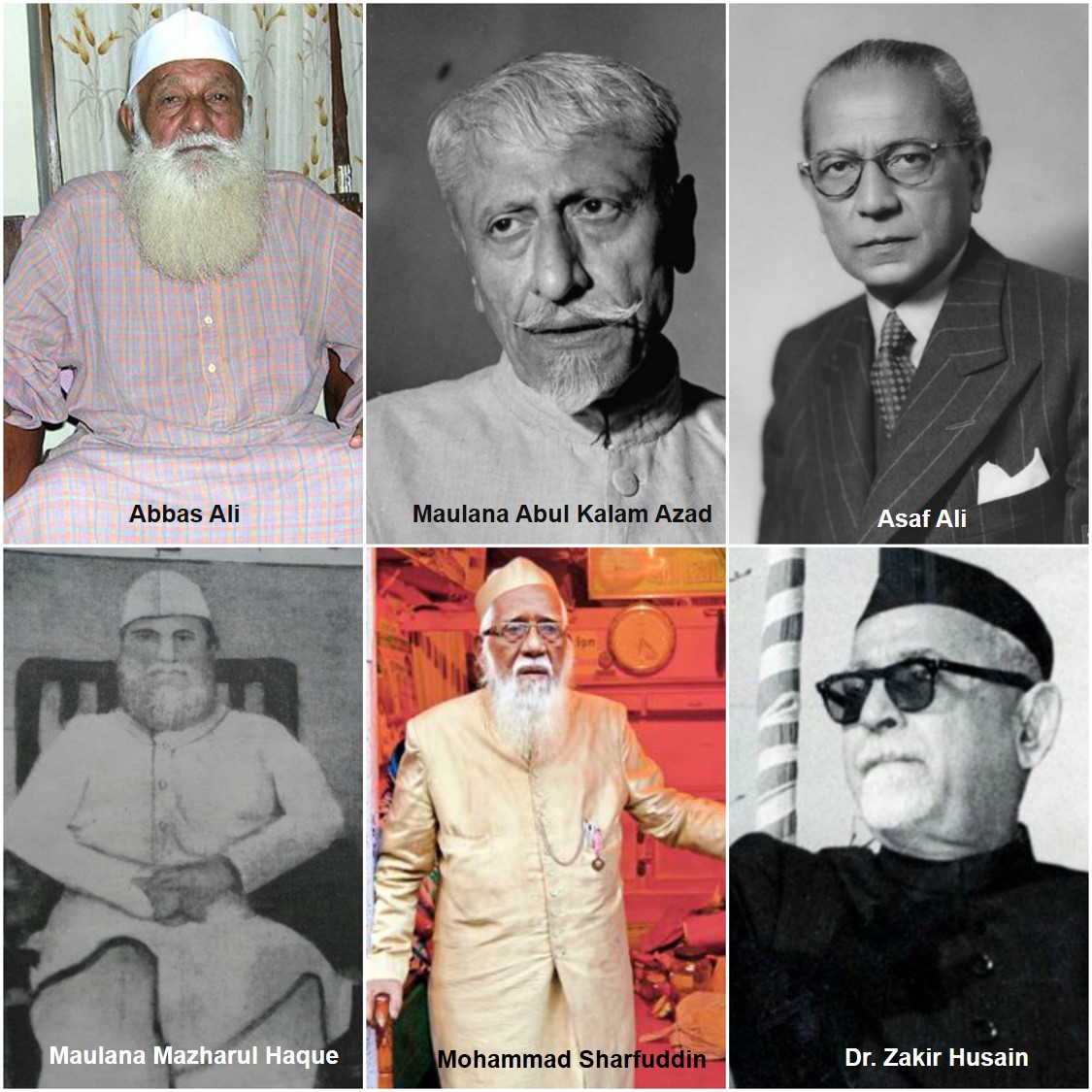आदि शंकराचार्य की विरासत संजोये, मंदिरों के शहर जोशीमठ के तमाम घरों, सड़कों और खेतों में दरारें आने से नागरिकों में भय व्याप्त है। लेकिन यदि सत्ताधीशों ने वैज्ञानिकों, भू-वैज्ञानिकों तथा पर्यावरणविदों की नसीहत को सुना होता तो एक पौराणिक शहर का अस्तित्व यूं खतरे में न पड़ता।
उल्लेखनीय है कि आज 21वीं सदी में जोशीमठ में जो संकट पैदा हुआ है उसकी आशंका वर्ष 1976 में एक शीर्ष नौकरशाह उजागर कर दी थी। उनकी अध्यक्षता में बने एक पैनल ने क्षेत्र में भारी निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी।
दरअसल, मिश्रा आयोग ने चेताया था कि जोशीमठ एक भूस्खलन के स्थल पर बसा है और बड़े निर्माणों का बोझ उठाने में सक्षम नहीं है। आयोग ने बड़ी संख्या में भवन निर्माण से परहेज रखने की सलाह दी। लेकिन उनकी सिफारिश को उत्तराखंड के सत्ताधीशों व प्रशासन ने अनदेखा किया। बीते दशकों में जोशीमठ में अंधाधुंध निर्माण कार्य हुए। रोप-वे के लिये भारी-भरकम पिलर बनाये गये। बताया जाता है कि ऊपर के पिलरों से दरार पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ । सवाल उठता है कि पहाड़ की कमजोर बुनियाद के बारे में चेताने के बावजूद आखिर बड़े पैमाने पर अव्यवस्थित निर्माण की अनुमति क्यों दी गई।
दरअसल, बड़ी पन- विद्युत परियोजनाओं के लिये सुरंग खोदने तथा ऑल वेदर राजमार्ग के विस्तार ने पहले से संवेदनशील ढलानों को अत्यधिक अस्थिर बना दिया। जिसका नतीजा आज बड़ी दरारों के रूप में सामने आ रहा है।
निस्संदेह, उत्तराखंड में तीर्थयात्रा और ट्रैकिंग सर्किट के लिये जोशीमठ महत्वपूर्ण पड़ाव है। साथ ही चीन की संवेदनशील सीमा के चलते इसका सामरिक महत्व भी अधिक है। यहां चीन सीमा की वजह से सेना की बड़ी छावनी स्थित है। सुरक्षा कारणों के चलते सेना की आवाजाही को सुगम बनाने के लिये सड़कों के बुनियादी ढांचे का उन्नयन भी जरूरी था । पर्यावरण विशेषज्ञ बताते हैं कि चमोली से लेकर जोशीमठ तक पूरा क्षेत्र आपदाएं झेल चुका है।
विशेषज्ञों का कहना है कि 2013 और 2021 की बाढ़ का इस इलाके में प्रतिकूल असर पड़ा था। दो साल पहले सर्दी के मौसम में एक हिमाच्छादित झील के फटने से करीब 204 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जिसमें ज्यादातर जलविद्युत परियोजना में काम करने वाले प्रवासी श्रमिक व कर्मचारी थे।
साथ ही संपत्ति का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। ऐसे वक्त में जब भूमि धंसने से जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, बचाव का तात्कालिक विकल्प नजर नहीं आता । प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने की चुनौती है। फिर उसके बाद उनके पुनर्वास की समस्या है।
लोगों ने जीवन भर की पूंजी जोड़कर घर बनाये हैं, घर छोड़ते वक्त उनकी आंखों में आंसू हैं। ऐसे में इस शहर को बचाने का यक्ष प्रश्न सामने है। दरअसल, बड़े निर्माण शुरू करने से पहले उस चट्टान का वैज्ञानिक आकलन जरूरी था जिस पर यह शहर टिका है। यह इलाका भूकंप की दृष्टि से भी संवेदनशील बताया जाता है।
विडंबना यह है कि इसके अलावा शहर के वर्षा जल व घरेलू जल निकासी के निस्तारण की पर्याप्त व्यवस्था यहां नहीं रही है। पानी पहाड़ के भीतर जाता रहा है। लोग यहां निर्माणाधीन पनबिजली परियोजना का निर्माण स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, जिसकी सुरंगों को खोदने के चलते संकट बढ़ने की आशंका जतायी जा रही है।
दरअसल, जोशीमठ भूगर्भीय हलचलों के चलते भी धंसने के प्रति संवेदनशील है। जो उपचारात्मक उपायों की तत्काल जरूरत बताता है। लेकिन इसको लेकर दीर्घकालिक रणनीति बनाने की जरूरत है। छोटे-छोटे टुकड़ों में समस्या का समाधान तलाशना चुनौती की गंभीरता को कम करने मे सहायक नहीं हो सकता। प्रयास हो कि स्थानीय लोगों की जीविका भी प्रभावित न हो।
इतना ही नहीं, जोशीमठकी चुनौती से सबक लेकर अन्य पर्वतीय शहरों की स्थिति की पड़ताल करने तथा उत्तराखंड की घाटियों में पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को लेकर फिर से विचार करने की भी जरूरत है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जोशीमठ की त्रासदी मानव निर्मित है। जिसके आलोक में अन्य पहाड़ी शहरों का भी मूल्यांकन करना चाहिए। ताकि फिर किसी दूसरे शहर को भय व अनिश्चितता में न जीना पड़े।