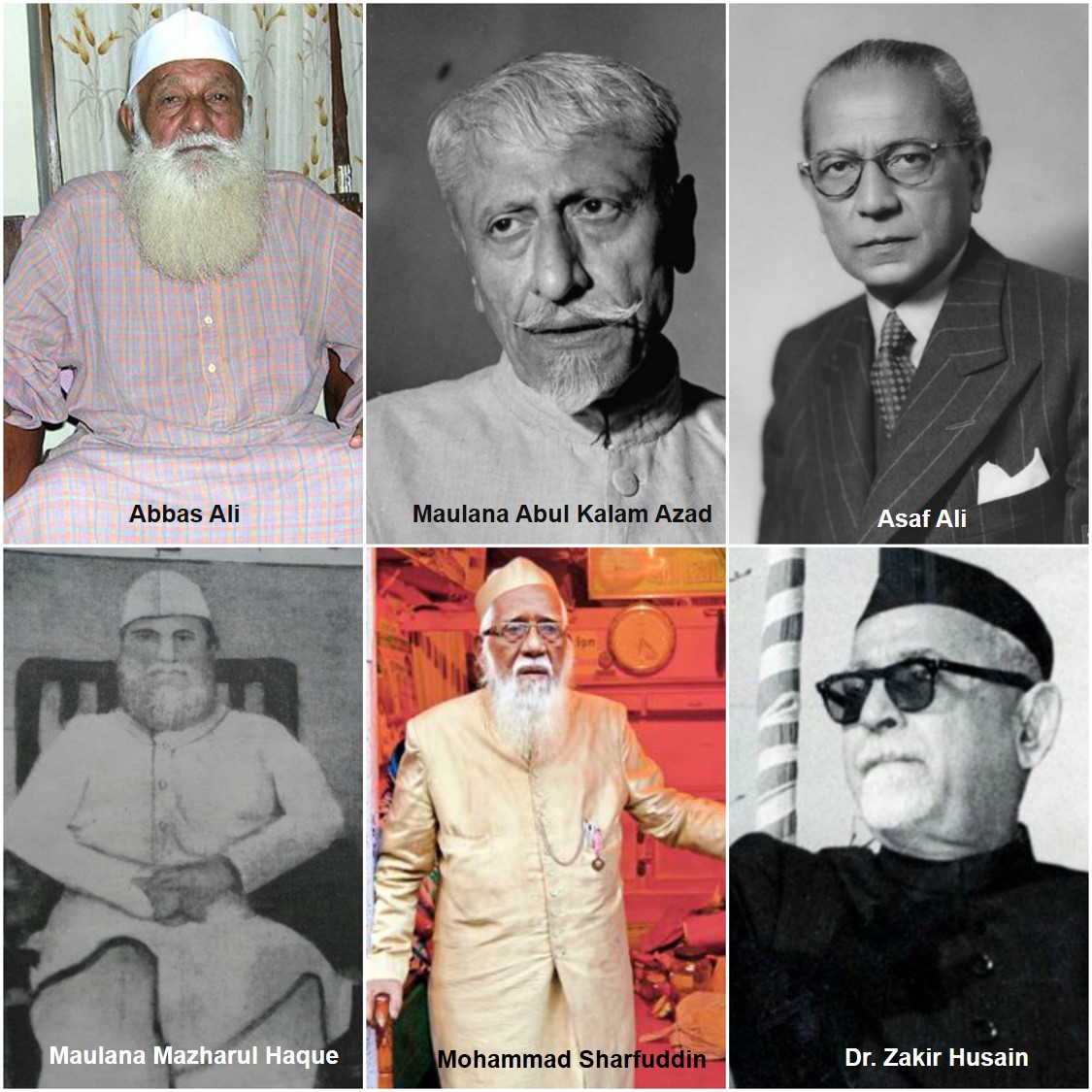हर तरह की आज़ादी की बुनियाद आर्थिक आज़ादी है, ये वाक्य अक्सर पढ़े लिखों के बीच चर्चा में आता ही है। अब आप जीवन के अपने अनुभव से इसे जोड़िये ! आपका बॉस आपको जाति, धर्म, रंग, जेंडर या नस्ल आदि की बुनियाद पर, या बस ऐसे ही कि वो बॉस है, आपको अपमानित करता है। क्या आप उसको उसके इस अपराध के लिए सज़ा दे या दिलवा सकते हैं ! क्या इस अपमान के कारण आप नोकरी को लात मार सकते हैं !
अधिकांश लोगों का ज़वाब होगा नहीं, अब दुबारा सोचिये कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना क्या सच में आज़ादी की बुनियाद है ?
अब आप अपने जी जीवन के कुछ और अनुभव लीजिये और अपने नैतिकता की परीक्षा कीजिये ! आपने अच्छे नंबर लाने के लिए चीटिंग की, क्योंकि अच्छा नंबर ही आपकी काबिलियत की बुनियाद है, हलांकि इसकी सच्चाई से हर कोई वाकिफ़ है। आपने अपने किसी नज़दीकी के प्रेम, सम्पदा या उसकी अवस्था का लाभ उठाकर ख़ुद की तरक़्क़ी की सीढ़ियां बनाईं, क्यों ! इसलिए न कि आपको आर्थिक रूप से मज़बूत होना था !
आपने अपने भाई या बहन से रिश्ते ख़राब किये या हुए, इसकी बुनियाद में भी संपत्ति है। ये वही भाई बहन हैं, जिनके लिए एक समय आप किसी की जान ले भी सकते थे और ख़ुद की दे भी सकते थे, फिर भी ऐसा हुआ, खोजियेगा तो इसकी बुनियाद में सम्पदा का मसला नज़र आएगा।
जिन जिन लोगों से आपके सम्बन्ध ख़राब हुए, उनकी भी पड़ताल कीजिये, जिन्हें आप पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, उनकी भी पड़ताल कीजिये, आप सबकी जड़ में सम्पदा को किसी न किसी रूप में देखेंगे।
एक और चिंतन है, अक्सर ऐसा बताया जाता है या हमें भी लगता है कि अगर पर्याप्त संपत्ति अर्जित कर ली जाए तो हमारी तमाम समस्यायों का समाधान हो जाएगा। ऐसे में उनको देखिये जिनके पास संपत्ति पहले से है। आप पाएंगे कि उनके जीवन में भी वो सारी समस्याएं हैं जिनका आप सामना करते हैं।
ऐसे में ये सवाल परेशान कर सकता है कि फिर हमारे दुख का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है ?
दरअसल आज से लगभग 3 हज़ार साल पहले ही दुख की इस अवस्था की पहचान कर ली गई थी। तबसे लेकर अभी दो सदी पहले तक इसका समाधान धर्म के दायरे में ढूढ़ने की कोशिश की गई। जैन, बौद्ध और वैदिक परंपरा के लोगों ने संपत्ति के ही त्याग का रास्ता अख्तियार किया और सुख के एक नए संसार की अवधारणा प्रस्तुत किया, जिससे मुक्ति और स्वर्ग की परिकल्पना वजूद में आई। मुक्ति में ये भाव निहित है कि जन्म ही दुख का कारण है इसलिए जन्म हो ही न, ऐसे प्रयास किये जाने चाहिए। दूसरी अवधारणा अच्छे कर्म के पश्चात अनंत जीवन की कल्पना करती है जिसमें स्वर्ग में आपका बंगला होगा वो भी सभी सुविधाओं से युक्त।
ईसाई और इस्लाम में सन्यास के बजाय धर्मपरायण जीवन जीते हुए स्वर्ग हासिल करने का रोडमैप मिलेगा। हलांकि सूफी और पादरी के रूप में सन्यास परंपरा यहाँ भी पैदा हो ही गयी।
धर्म के रास्ते सभी सुखी नहीं हो सकते, एक तो संपत्ति या मोह माया का त्याग सभी नहीं कर सकते, ऐसा हो जाये तो त्यागियों का भी जीना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे, जिन्होंने त्याग किया, उनको भी क्या मिला, इसका कभी भी पता नहीं चलता।
पर एक बात तो साफ़ है कि धर्म ने निजी सम्पदा को दुख के कारण के रूप में पहचाना, ये अलग बात है कि जिस साफगोई से ये बात मैं कह रहा हूँ, धर्म ऐसे नहीं कहते। लेकिन धर्म वो समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाया जो सबके लिए सहज हो और दिखाई भी पड़े। इसका एक बड़ा कारण ये है कि धर्म उस दौर में वजूद में आये जब निजी सम्पदा मनुष्यता को लगातार समृद्ध कर रही थी। निजी सम्पदा एक तरफ़ तो समृद्धि के कीर्तमान स्थापित कर रही थी, दूसरी तरफ इसी पर आधारित नई तहज़ीब भी पैदा कर रही थी, धर्म भी इस तहज़ीब का हिस्सा था और हिस्सेदार भी।
जाहिर सी बात है, असमानता को निजी सम्पदा की दुनिया के बाई प्रोडक्ट के रूप में सामने आना ही था, तो आया। मनुष्य के दुख और बेचैनी का कारण लगातार खोजा जाता रहा और अभी 19 वीं सदी में इसका एक वैज्ञानिक समाधान ढूढ़ा गया। समाधान ये निकला कि सम्पदा का परित्याग नहीं करना है बल्कि निजी सम्पदा को सामूहिक सम्पदा में बदल देना है, सम्पदा सामूहिक, दायित्य सामूहिक, सृजन सामूहिक और उपभोग भी सामूहिक। दो लाइन में कही गयी ये बात दरअसल गहन मीमांसा की मांग करता है, लेकिन ये मीमांसा आपको नजी और सामूहिक दोनों रूपों में करना है, फिर सोचना है कि निजि स्वामित्व पर खड़ी आज की व्यवस्था जो जीवन और पर्यावरण दोनों को निगल जाने पर आमादा है, उसे कैसे बदला जाए !
लेकिन कुछ काम अभी करना है। आपके बहुत से संबंध निजी सम्पदा अर्जित करने में या अर्जित किये हुए को बचाने में बिखर गए हैं, उन्हें समेटिये !बस उनके साथ कुछ वक्त गुज़ारिये, कभी सुख दुख की बातें फोन पर ही कर लीजिए, अगल बगल के लोगों को कभी कभी चाय पर बुला लीजिये, बगल के परिवार के बच्चों के साथ कभी खेल लीजिये, स्कूल कॉलेज़ के मित्रों, शिक्षकों को भी कभी कॉल कर लीजिए। इसके साथ ही सम्पदा के पीछे भूत बनकर भागना भी छोड़ दीजिए।
ये बातें कहने सुनने में बहुत सरल हैं, लेकिन जब आप अमल करेंगे तो क़दम क़दम पर मुश्किलें मिलेंगीं, फिर भी इसे करते रहना होगा, इसलिए नहीं कि इससे आप किसी पर कोई उपकार कर देंगे, बल्कि इसलिए कि पूँजीवाद की तमाम कोशिशों के वावजूद ऐसा करने से आप मानसिक रोगी होने से बच जाएंगे। तमाम कठिनाइयों के बावजूद अगर हम इतना कर पाते हैं, करते जाते हैं तो व्यापक सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए भी ज़मीन तैयार होने लगेगी।
अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अकेलापन, उदासी, अवसाद और अनिद्रा तो आपके मुन्तज़िर हैं ही। पूँजीवाद आपको खींच खींच कर, पीट पीट कर अब यही देने वाला है। हाँ, बचने या न बचने का फैसला अभी भी आपके हाथ में है।
(डॉ. सलमान अरशद)