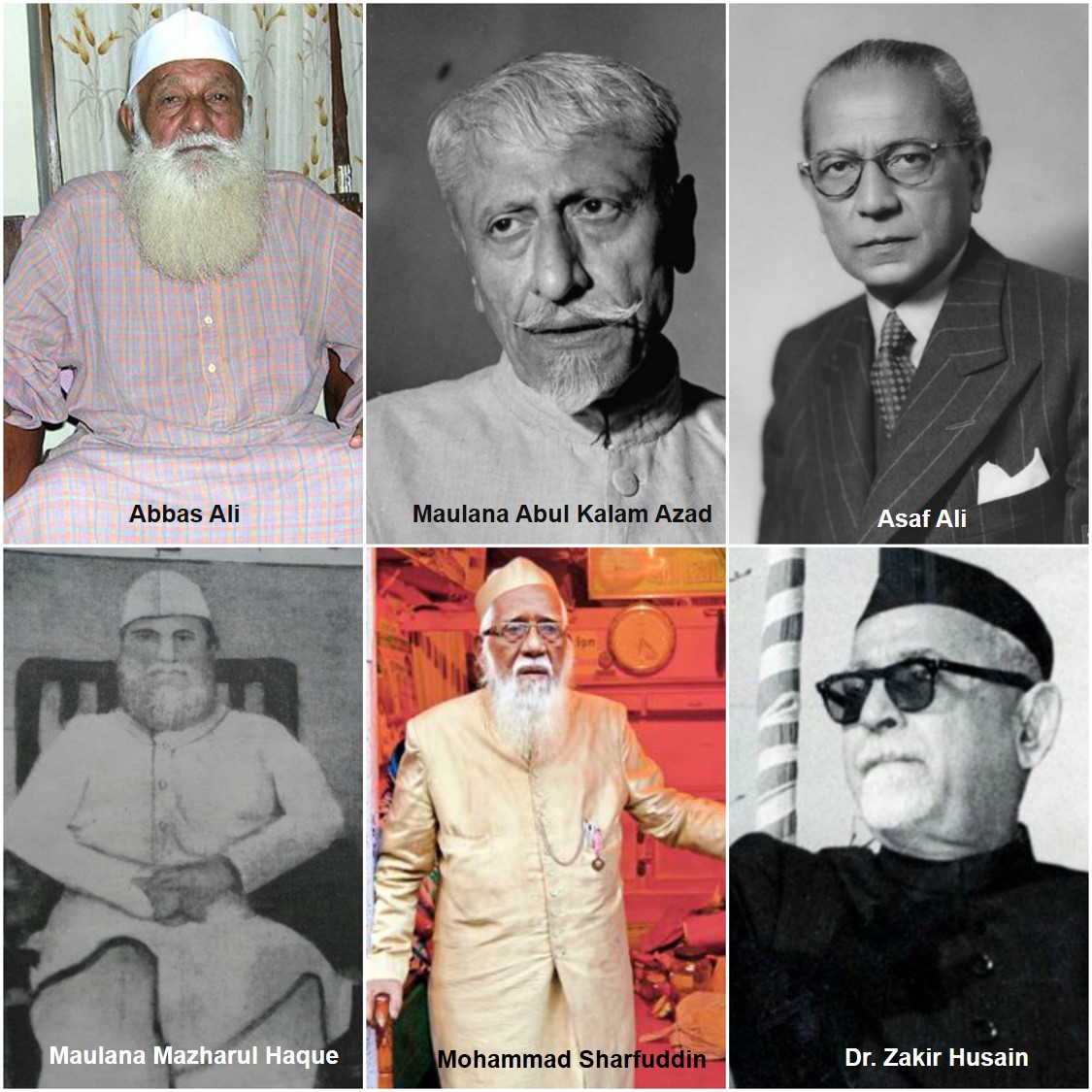यूपी की चुनावी राजनीति में जातीय समीकरण एक सच्चाई है. पहले ऐसा नहीं था. कम्युनिस्ट पार्टियां और सोशलिस्ट पार्टी का जनाधारा ज्यों-ज्यों खिसकता गया, तभी धर्म और जाति की राजनीति को अपना सर उठाने का मौका मिला. पहले राममंदिर आंदोलन विहिप ने शुरू किया, जिसे भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी ने लपक लिया. उसके बाद धीरे-धीरे बसपा का उदय हुआ जो जातीय समूहों की एक गोलबंदी थी.
ये भी पढ़ें: सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर…
बाद के दिनों में बसपा से जुड़े क्षत्रप मायावती को झटका देते हुए अपने जतीय समूहों की गोलबंदी करके खुद नई-नई पार्टियां बना लिए और सत्ता में भागीदारी के लिए जब भी मौका मिला बड़े दलों से समझौता कर सत्ता सुख भोगने लगे. उनके मतदाता भी अपने नेता की कलाबाजी देखकर आत्ममुग्ध होते रहे. अब महंगाई, बेरोजगारी से परेशान लोगों की नींद टूटी है. कोरोना के पहले और दूसरे लाॅकडाउन ने रोजगार धंधा चौपट कर दिया है. छोटे-मोटे काम करके जो अपनी जीविका चलाते थे, उनकी भी हालत खस्ता है.
कोरोनाकाॅल में ही तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब व हरियाणा के किसान भी गोलबंद हुए और दिल्ली बाॅर्डर पर नौ महीने से डेरा डाले हैं. दूसरे राज्यों के किसानों का समर्थन मिलने से उनका हौसला बढ़ा है. इसका सकारात्मक पहलू यह है कि किसान आंदोलन ने जाति और धर्म के दायरे को तोड़ा है, लेकिन चुनावी राजनीति की दृष्टि से इसका क्या असर होगा, इसे देखना अभी बाकी है. पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में तो किसान नेता अपनी उपस्थिति दर्ज कराए थे और उसका परिणाम भी सामने है.
किसान आंदोलन अब एक सच्चाई बन गया है. उनकी समस्याओं को नकार करके किसी भी राजनीतिक दल के लिए आज की तारीख में चुनावी रणनीति बनाना संभव नहीं है. और यही किसान आंदोलन की सफलता है. शायद देश में कोई दूसरा ऐसा आंदोलन नहीं हुआ है, जो नौ महीने से अधिक समय तक चला हो. किसानों को बदनाम करने की बहुत कोशिशें की गईं. उन्हें आतंकवादी तक कहा गया और हाई-वे को खोदकर उनके रास्ते में लोहे की कीलें बिछा दी गईं. जाड़े में उनके ऊपर वाॅटर कैनन से पानी फेंका गया लेकिन सभी जुल्मों को झेलते हुए वे दिल्ली बाॅर्डर पर डटे हैं.
सत्ता पक्ष या विपक्ष किसी के लिए भी अब किसानों को छोड़कर चुनावी दंगल में कूदना आत्महत्या करने के समान होगा. यही कारण है कि यूपी की योगी सरकार भी अब परेशान है. खेती-किसानी करना अब महंगा हो गया है. खाद-बीज के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है. बिजली भी महंगी है. उत्तर प्रदेश में बिजली प्रति यूनिट देश में शायद सबसे अधिक है. किसानों के बकाया गन्ना का मूल्य भी सरकार के लिए सिरदर्द बना है.
इस माहौल में यूपी में राजनीतिक दल चुनावी समर में कूदने के लिए अपने-अपने अखाड़े में रियाज शुरू कर दिए हैं. सपा, बसापा और आम आदमी पार्टी ने खुद अपने दम पर चुनावी समर में कूदने का ऐलान किया है. “भूराबाल” के अपने नारे को भूलकर बसपा अब प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन करने में जुटी है. कांग्रेस पार्टी भी अपने खोए हुए जनाधार को पुन: समेटने की जुगत में लगी है. उधर, बसपा के पारम्परिक वोटों पर भाजपा नज़र गड़ाए बैठी है. इसमें उसे बहुत कुछ सफलता भी मिली है.
इस चुनावी शोर के बीच महंगाई व बेेरोजगारी का सवाल बहस के केंद्र में ही नहीं आ रहा है. इसमें मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है. मुख्यधारा की प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया सत्ता द्वारा खड़ा किए गए नैरेटिव पर ही बहस करने में दन-रात एक कर दी है. मीडिया फिलहाल अफगानिस्तान पर बहस कर रही है लेकिन अपने घर की समस्याओं से उसे कोई मतलब नहीं है. मीडिया को यह चिंता है कि रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की काबुल में तालीबान ने कोड़े से पिटाई की है, लेकिन भारत में पत्रकारों की दशा क्या है ? इस सवाल पर वे चुप्पी साध जाते हैं. हमें समस्या को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है. दमन चाहे जहां भी हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं.
छह महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है. ऊंट किस करवट बैठेगा, इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. राजनीतिक समीक्षकों की अभी से यूपी के चुनाव पर नज़र है. सबको पता है कि इसके नतीजे का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा. यही करण है कि वोटों के बनते-बिगड़ते समीकरणों के बीच लोगों की आर्थिक बदहाली चुनावी नतीजे को प्रभावित करने में कितना असरदार साबित होती है, यह जानना महत्वपूर्ण होगा.
सुरेशप्रताप