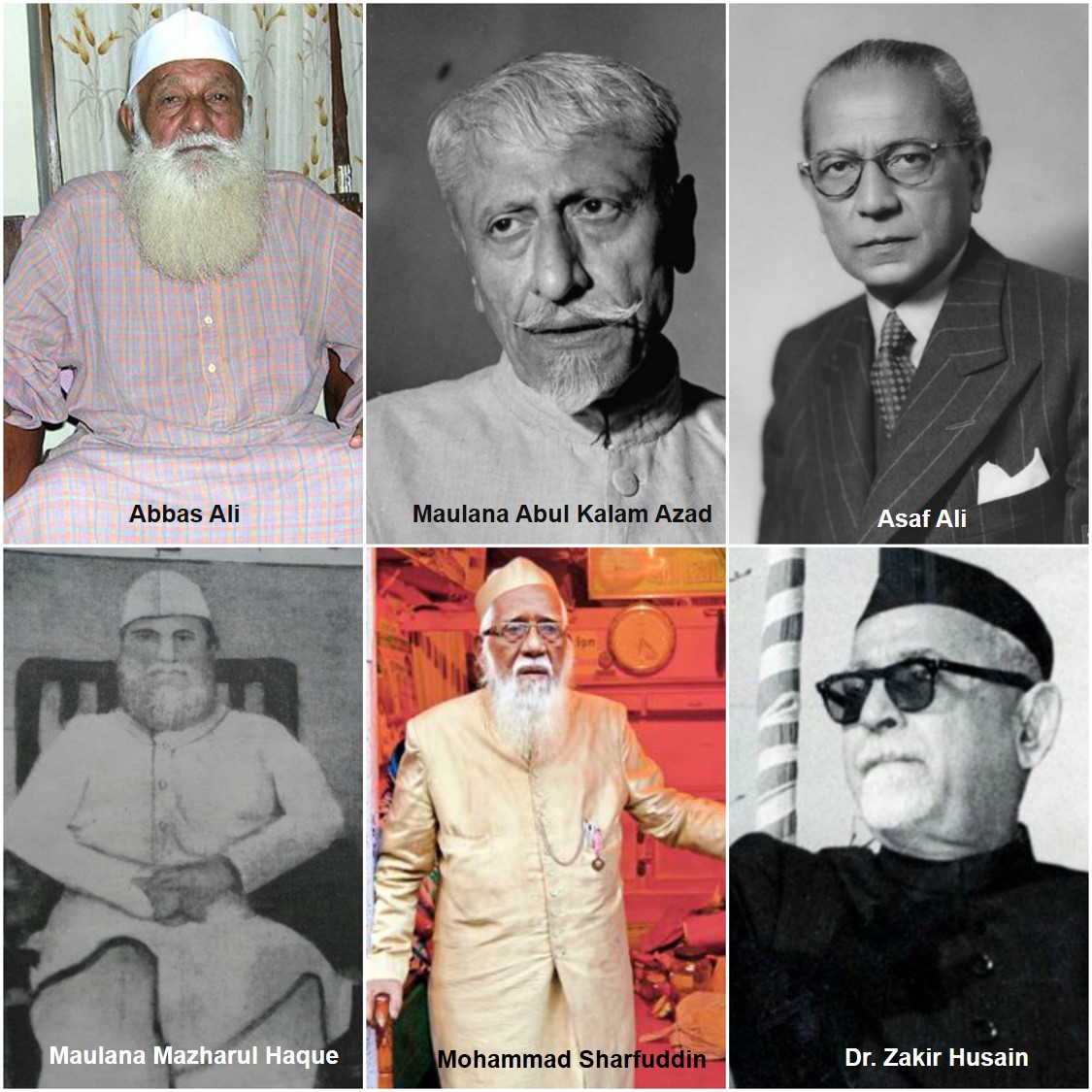कथा वाचन की परंपरा हिंदुस्तान में काफ़ी पुरानी है। जो संदर्भ हमें उपलब्ध होते हैं उनमें महाभारत और हर्ष चरित का ख़ासतौर पर जिक्र किया जा सकता है।
महाभारत(1.2.13.3) में कहा गया है कि वनों में रहने वाले कथक मधुर स्वर में कथा सुनाते हैं। हर्ष चरित् (I/73-77)में भी कथक का संदर्भ मिलता है।
इसी कड़ी में मानसोल्लास(11वीं शताब्दी) और संगीत रत्नाकर(13वींशताब्दी) का उल्लेख किया जा सकता है। मानसोल्लास कथक विनोद के रूप में और संगीत रत्नाकर नरत्नाध्याय में कथक का उल्लेख करता है।
एक कहावत है ‘कथा कहे सो कथिक कहावे’ माने जो भावपूर्ण ढंग से कथा कहे वह कथिक है। कथा कहने की यह शैली नृत्य से कब अभिन्नता से जुड़ी कहना मुश्किल है।
दस्तावेजों को खंगालने पर इसकी जड़ें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर से जुड़ती हैं। इलाहाबाद की हड़िया तहसील में एक गाँव है चुलबुला। ईश्वरी प्रसाद मिश्र इस गाँव के रहने वाले थे और पेशे से कथिक थे। एक रोज भगवान कृष्ण ने उन्हें स्वप्नदर्शन देकर कथक के प्रचार प्रसार का निर्देश दिया।
उन्होंने इस आदेश का अनुपालन करते हुए लख़नऊ में बसना तय किया और कथक के पहले नर्तक बने। उन्ही के माध्यम से कथक ने पौराणिक कथा वाचन से दरबारी नृत्य तक का सफ़र तय किया। ईश्वरी प्रसाद की अगली दो पीढ़ियों ने नृत्य की इस शैली को लख़नऊ के नवाबी दरबार तक पहुँचाया।
कृष्ण के नाम पर ईश्वरी प्रसाद ने इसे ‘नटवरी नृत्य ‘कहा। नृत्य की बारीकियों पर एक किताब लिखी और अपने तीनों बेटों को नृत्य की इस विधा में प्रशिक्षण दिया।
उनके पुत्र अङ्गु जी ने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने पुत्रों प्रकाश,दयाल और हीरालाल को कथक में पारंगत किया।यही तीनों भाई नृत्य की इस शैली को अवध के दरबार तक लेकर आये। इनके माध्यम से कथक पौराणिक आख्यानों से दरबारी नृत्य की शैली में तब्दील हो गया।
इसके बाद लख़नऊ और कथक एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े कि लखनऊ नृत्य की इस शैली का पर्याय हो गया। कथक का विकास लख़नऊ के नवाबों की छत्र छाया में हुआ जिसके असल झंडाबरदार नवाब वाज़िद अली शाह थे। चर्चा है कि नवाब शुजाउद्दौला के समय में रोज़गार तलाशते अनेकों कलाकार फैज़ाबाद पहुँचे। इनमें साजिंदे और तवायफें भी शामिल थे।
आसफ़ुद्दौला के लख़नऊ आने पर ये कलाकार रोजगार के लिए नवाब के साथ लख़नऊ आ बसे।
नवाबों को लुभाने और उनका मनोरंजन करने के उद्देश्य से कथक के पौराणिक आख्यानों को प्रेमाख्यान में बदला गया जिससे दरबार मे उन्हें पेश कर रोजी कमाई जा सके। नाचने गाने की कला में माहिर तवायफों ने इस नृत्य शैली को अपना लिया और इसे मुजरे के रूप में पेश करने लगीं। इस तरह कथक नृत्य की एक ख़ास शैली के रूप में विकसित हुआ और मुजरे से अभिन्नता के साथ जुड़ गया।समय के साथ लख़नऊ का कथक घराना कालका बिंदादीन घराना कहलाया।