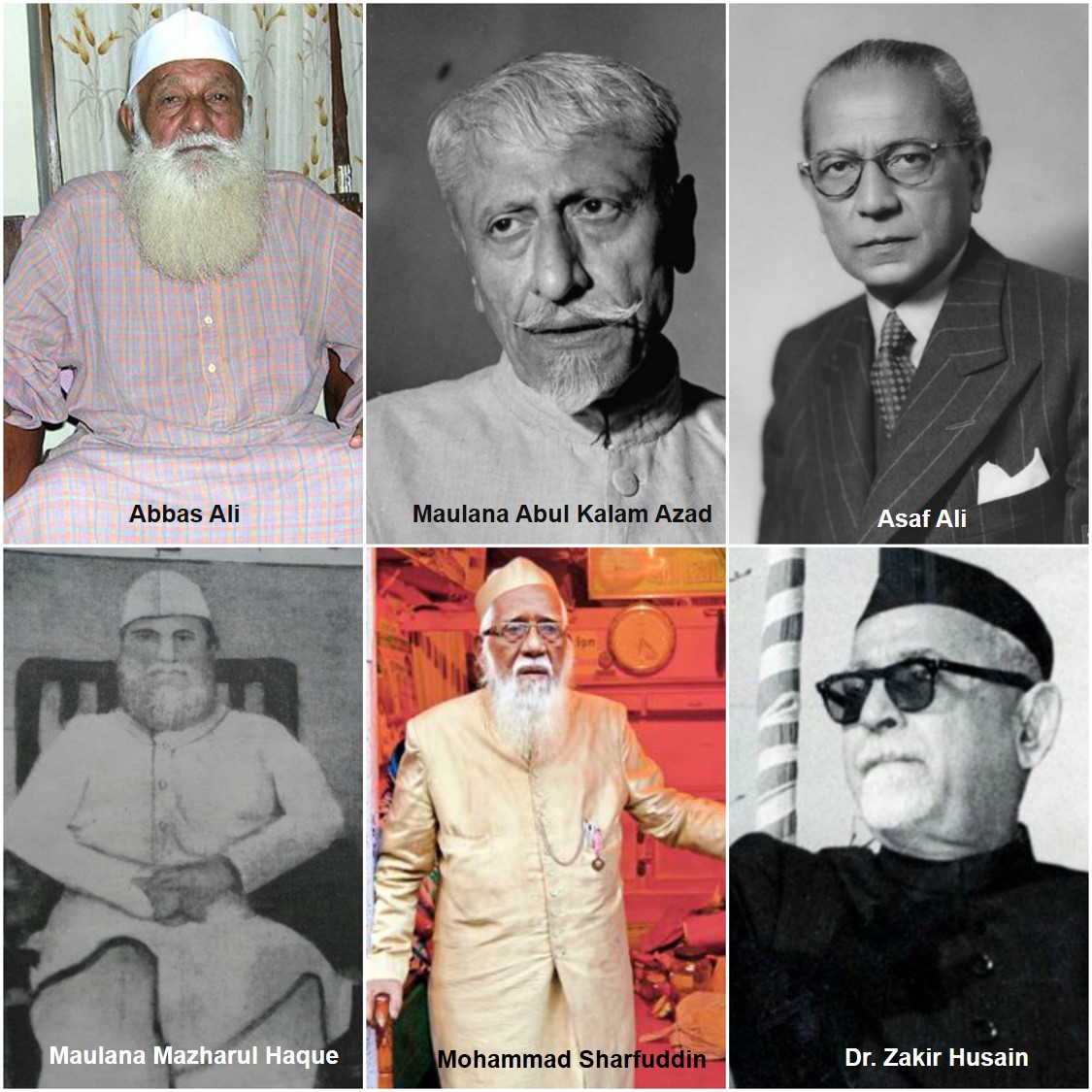बनारस के किस्से और लोग, सलाम चचा और हीरा लाल वाल्मीकि
सलाम चाचा, पूरे मुहल्ले के चाचा थे। उन्हें मैं पूरी अकीदत के साथ सलाम करता हूं। बरसों तक मैं उनकी आँखों से ही उन्हें पहचानता रहा। क्योंकि मुँह और नाक पर वे हमेशा गमछा बॉंधे रहते थे।साफ सफाई के औजार संभाले उनकी गंदगी ढूँढती आंखें ही हमें हमेशा दिखाई पड़ती थीं। जाड़ा, गर्मी और बरसात कोई भी महीना हो,सलाम चचा सुबह सात बजे ड्यूटी पर आ जाते और उनके कन्धे पर टंगी मशक हमारे कौतुक का कारण होती।
बहुत दिनों तक मुझे मशक कोई जानवर जैसी दिखाई देती थी।मशक में सरकारी नल से पानी भरने की समूची प्रक्रिया हमारी उत्सुकता के केन्द्र में होती थी। चचा नालियों की सफ़ाई को काम की तरह नहीं बल्कि धर्म की तरह करते थे। मशक में पानी भरने के उनके कर्मकांड को मेरी जिज्ञासा शुरू से अंत तक निहारती रहती।कन्धे पर मशक टांगें, गमछे से मुंह बॉंधे सलाम चचा हमें कोई जादूगर से लगते थे।
सलाम चाचा भिश्ती थे। नालियों की सफ़ाई उनका काम था। उनकी मशक कौतुहल जगाती थी।अगर आप किसी बड़े बकरे को उलटा कर कन्धे पर टॉंग ले तो वह मशक की शक्ल में ही दिखेगा। इसी मशक की धार से पानी डाल सलाम चाचा मुहल्ले की गंदी बजबजाती नालियों को फ़ौरन चमका देते। मशक पानी ढोने वाला चमड़े का बड़ा थैला होता था। जो बकरे की खाल का बनता था। उसे लीकप्रूफ बनाया जाता था।
विकास की रोशनी जब मुहल्ले पर पड़ी तो नालियाँ अण्डरग्राउण्ड हुईं। पर सलाम चाचा भी तस्वीर से ग़ायब हो गए। उस वक्त तक बनारस में कुल अस्सी भिश्ती नगर महापालिका के रिकॉर्ड पर दर्ज थे जिनके ज़िम्मे शहर की गंदी नालियों की सफ़ाई थी। 1997 से भिश्ती और मशक को बनारस नगर निगम ने काम से हटा दिया। लेकिन सलाम चचा भिश्ती प्रणाली के बंद होने से पहले ही रिटायर हो गए थे।
पीढ़ियों से भिश्ती का काम कर रही ये जमात अब बेरोज़गार है। सलाम चचा के परिवार के लोग अब गधे पालने लगे। इस बात से आप हतप्रभ हो सकते हैं कि बनारस की पतली पतली गलियों में कूड़ा और मलबा उठाने के लिए गधे बतौर कर्मचारी रखे जाते थे या यूं कहिए कि जिन लोगों के पास गधा था वह अपने गधे की वजह से नगर निगम में नौकरी पा जाते थे। उन्हें तनख्वाह के रूप में गधे की ख़ुराकी भी मिलती थी जिसे उसके मालिक की तनख्वाह में शामिल कर दिया जाता था। मैनें पता किया तो मालूम चला कि दो गधे कर्मचारी के तौर पर वहॉं आज भी नौकरी पर हैं।
अक्सर सलाम चाचा मुहल्ले की सफ़ाई के बाद मेरे घर के चबूतरे पर आकर बैठ जाते और अम्मा उन्हें चाय भिजवातीं।कभी कभी उनका खाना पीना भी हमारे यहॉं ही होता था। सलाम चचा पुश्तों से भिश्ती का काम करते थे। वे बातचीत नफ़ीस करते। साफ़ सुथरे आदमी थे। हर किसी की मदद को हमेशा तत्पर रहते। मुझे बचपन में यह सवाल हमेशा परेशान करता था कि सारे मुहल्ले को साफ-सुथरा रखने वाले सलाम चचा शहर के बाहर गंदी बस्ती में तमाम वंचनाओं के साथ गुजर-बसर करने को आखिर क्यों मजबूर थे?
बदलते समय के साथ समाज में भिश्ती भी वक्त की गहराइयों में गुम होता गया।आज की पीढ़ी तो शायद भिश्ती को जानती भी नहीं होगी। उसके लिए यह यकीन करना मुश्किल होगा कि समाज में कोई ऐसा भी आदमी रहा होगा, जो चमड़े के थैले में पानी का परिवहन करता था। वह चौराहों पर पानी भी पिलाता।
शादी ब्याह में पानी लाने की ज़िम्मेदारी उसी की होती। भिश्ती,उत्तर भारत और पाकिस्तान में पाई जाने वाली मुस्लिम जनजाति थी। इनका मूल काम मशक से पानी ढोना था। मध्यकाल में सैनिकों को पानी पिलाने और पानी ढोने वालों को भिश्ती कहा जाता था और तभी से ये शब्द पूरे मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में प्रचलित हुआ। भिश्ती फ़ारसी शब्द ‘बहिश्त’ से बना है, जिसका अर्थ जन्नत होता है।
पुराने जमाने में यह कहा जाता था कि लोगों की प्यास बुझाने वाला बिहिश्त यानि स्वर्ग जायेगा। इसलिए इनका नाम भिश्ती पड़ गया। Rudyard Kipling की कविता “Gunga Din” का पात्र एक भिश्ती ही है। भिश्ती अरब क्षेत्र के अब्बासी समुदाय से आते थे। अब्बासी समाज की पूरे देश में कोई साढ़े चार करोड़ व उत्तर प्रदेश में दो करोड़ की आबादी है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत में भिश्तियों का आगमन मुगल सेनाओं से साथ हुआ था और वहीं से ये पूरे भारत में फैल गए।
भिश्तियों के साथ ही साथ मशक भी अब इतिहास की चीज़ हो गयी है।मशक की बनावट रोचक थी। मशक अलग-अलग आकारों में बनती थी।छोटी मशक हाथ में उठाई जाती थीं। बड़ी मशकें कंधे पर टांगी जाती थी। बड़ी मशक ले जाने वालों को ‘माश्की’ कहते थे।
भिश्ती हर काल में लोगों को राहत देने और मदद पहुंचाने वाली बिरादरी मानी गई। युद्ध में हारते हुमायूं की जान भी एक भिश्ती ने ही बचाई थी। 1539 में बक्सर के चौसा में मुगल बादशाह हुमायूं और अफगानी शासक शेरशाह के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई,वो जान बचाने के लिये गंगा में कूद गया।
हुमायूँ तैरते-तैरते थक गया।उसे लगा कि वो अब डूब जाएगा, तभी उसकी नजर एक नाविक पर पड़ी। हुमायूँ ने नाविक से मदद की गुहार लगाई। नाविक निजाम नाम का एक भिश्ती था। नाविक ने हुमायूं की जान बचा ली,जिसके बाद हुमायूं ने जान बचाने वाले नाविक निजाम को एक दिन के लिए राजा बनाने का वादा किया। बाद में बनाया भी।
भिश्ती और मशक की ये दास्तां लंबी और ऐतिहासिक है पर मेरे लिए इसका वजूद इस दास्तां के मूल पात्र सलाम चाचा से है। चाचा के भीतर गजब की विवेचना शक्ति थी। धार्मिक और समाजिक विवादों पर वे दार्शनिक दृष्टि रखते थे। अपने सफ़ाई कर्म पर उन्हें कभी कोई हीन भावना नहीं थी। वे पचास के हो गए थे पर बदन में कोई झुर्री नही थी।
चचा मुद्दों पर तन कर बात करते थे। वास्तव में वे सफ़ाई को कोई पाप या नापाक कर्म नहीं मानते थे। उनकी दलील होती “हम गंदगी के दुश्मन हैं। ऊपर वाले ने हमें इस काम पर लगाया है।” वे मानते थे कि सफ़ाई ही ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता है। चचा अक्सर कबीर का कहा दुहराते, “न्याहे धोए क्या भया। जो मन मैल न जाय। मीन सदा जल में रहे। धोए बास न जाए।”
स्वभाव से सलाम चचा बेहद सहज और विनम्र थे। हालांकि बनारस में सफ़ाई कर्मियों में भी गजब का ताव होता है। जब वे सफ़ाई के काम में लगे होते हैं, उस वक्त काशी नरेश की सवारी भी सामने आ जाय तो भी हटते नहीं हैं। इसकी झलक आचार्य शंकर ने भी देखी थी। उनकी आँख भी एक सफ़ाई वाले ने ही खोली थी।
अद्वैत के प्रतिपादक शंकराचार्य को अद्वैत का असली ज्ञान बनारस में एक सफ़ाई कर्मी से ही हुआ।तब तक शंकराचार्य भी मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद, दूरी और छुआछूत के चक्रव्यूह का साधन बने हुए थे।एक दिन आचार्य शंकर बनारस में गंगा स्नान कर लौट रहे थे। ब्रह्म मूहूर्त का वक्त था।
नगर की सफ़ाई के इंतजाम में लगा एक सफ़ाईकर्मी झाड़ू के साथ सड़क की सफाई कर रहा था।बीच रास्ते में सफ़ाई वाले को देख जगदगुरू का मन अरुचि से भर उठा।वे आदेशात्मक ढंग से बोले, “मार्ग से दूर हटो।”
सफाईवाला भी पहुँचा हुआ बनारसी था। बोला, “महाराज देह से देह को दूर करना चाहते हैं या आत्मा से आत्मा को? यदि पहली बात है? तो देह जड़ है, महाराज। उससे दूर क्या? पास क्या? और अगर दूसरी बात ठीक है, तो महाराज, आत्मा एक है। फिर एक से दूसरे की दूरी कैसी?” शंकराचार्य की आंखें खुल गयीं। ज्ञान का जो सार उन्हें बड़ी-बड़ी पुस्तकों, भ्रमण और साधना से न मिल सका, उसे एक सफ़ाईकर्मी ने दे दिया था। उसके बाद ही शंकराचार्य ने अद्वैत को नई रोशनी में देखा।
मैं खुशनसीब हूँ कि शंकराचार्य को रास्ता दिखाने वाले इस समाज को मुझे बेहद करीब से देखने और समझने का मौका मिला। बनारस में सलाम चचा थे तो लखनऊ पंहुचने पर मुझे हीरालाल वाल्मीकि मिले। बहुत ही विनम्र और यारबाज।अपने इसी स्वभाव से हीरालाल वाल्मीकि मेरे बृहत्तर परिवार के सदस्य बन गए। लखनऊ के मेरे घर के बाहर डाली बाग की उस सड़क की सफ़ाई का जिम्मा हीरालाल के पास था जो सूबे में पुलिस के सबसे बड़े हॉकिम डीजीपी के दफ़्तर से गोमती नदी तक जाती।
नींद खुलते ही सुबह-सुबह जब मैं अपने गेट के पास अख़बार लेने जाता तो सबसे पहली मुलाक़ात इन्ही हीरालाल से होती।पहले मेरे लिए यह रहस्य था कि रोज़ नमस्कार करने वाले आख़िर ये सज्जन हैं कौन? बाद में पता चला ये हीरा लाल हैं, नगर निगम के सफ़ाईकर्मी। फिर जैसा होता है कि रोज रोज़ की “जय रम्मी” से वे हमारी मित्र मंडली में शामिल हो गए। सुबह मैं अक्सर लॉन में बैठकर अख़बार पढ़ता। इस बीच वे सफ़ाई का अपना काम पूरा कर मेरे पास आते। हाल चाल होता।
एक प्याली चाय पीते और मुहल्ले भर की खबर बताते, फिर चले जाते। बदले में आए दिन वे सफ़ाई के बाद मेरी पटरी और गेट पर चूना छिड़कवा देते। चूने की यह लाईन अक्सर सरकारी समारोह और विवाह आदि में ही दिखाई पड़ती, जो मेरे यहॉं हीरालाल रोज़ करा देते थे। मेरे घर पर हर पखवाड़े कोई न कोई उत्सव मनाया ही जाता था। सो हीरालाल सड़क और पटरी हमेशा चमका कर रखते।
ये बात साल 2002 की होगी। 27 सितम्बर को मेरा जन्मदिन होता है।26 की रात बच्चों और मित्रो ने भोजन भात रखा। सोते-सोते देर हुई तो 27 की सुबह देर तक सोता रहा। नींद खुली तो बैण्ड की आवाज़ से। मैं अचकचाया।आखिर सबेरे-सबेरे यह बैण्ड बाजा कहॉं से? मेरा सरकारी घर लबे सड़क था।सामने की सड़क ही भैंसाकुण्ड (लखनऊ का श्मशान घाट ) जाती थी। मुझे लगा कोई पुण्यात्मा गत हुए और उन्हें गाजे बाजे के साथ ले ज़ाया जा रहा है।
लेकिन बैण्ड की आवाज़ कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही थी। तब पता चला कि यह आवाज़ तो मेरे घर से ही आ रही है। बाहर आकर मैंने ‘ड्राईव वे’ में जो कुछ देखा उससे हतप्रभ था।’ड्राईव वे’ के दोनों ओर क़तार से वर्दी धारी बैण्ड पार्टी के पॉंच-पॉंच लोग खड़े थे और बीच में हीरालाल वाल्मीकि एक छड़ी ले ज़ुबिन मेहता की तर्ज़ पर उन्हें निर्देशित कर रहे थे। धुन थी “तुम जिओ हज़ारों साल, साल के दिन हो पचास हज़ार।” मैं कुछ समझता, इससे पहले हीरालाल एक बुके लेकर मेरी ओर बढ़े। मेरी आँखों में आह्लाद के आंसू थे।दिल हीरालाल के लिए धड़क रहा था और हीरालाल मेरे गले से लिपटे हुए थे।
उसी रोज़ मुझे पता चला कि नगर निगम में सफाईकर्मियों का भी कोई बैण्ड होता है। हीरालाल उसके बैण्डमास्टर थे।पर्व ,प्रयोजन और शादी ब्याह के लिए इस बैण्ड की बुकिंग होती थी।बैण्ड पार्टी के सभी सदस्यों को मैंने जलपान कराया, रात का केक खिलाया।हीरालाल के इस असीम स्नेह ने उन्हें मेरे परिवार का अभिन्न सदस्य बना दिया।
वे वाल्मीकि समाज के नेता भी थे। अब भी वे मेरे जीवित सम्पर्कों में हैं।लिखने से पहले मैंने उनके कुशल क्षेम के लिए फ़ोन किया। उन्होंने बताया बुजुर्ग हो गया हूँ। घर पर ही रहता हूँ गुरू जी कोई आदेश हो तो बताईए। मैंने कहा “कोई वजह नहीं। कोविड काल में हाल चाल के लिए फ़ोन किया था।आपकी याद आ गयी।” हीरा लाल पुरानी यादों में खो गए।
लखनऊ से जब मैं दिल्ली आया तो एक रोज़ हीरालाल का संदेश मिला “बेटी की शादी है आपको ज़रूर आना है।” बिना मुझे सुने हीरा लाल आने की ज़िद पर अड़े रहे। मैं गया भी। व्यस्तता ज़्यादा थी। एक जहाज़ से गया, दूसरे से आया।
हवाई अड्डे पर मित्र Naveen Tewari मुझे लेने आए। उन्होंने पूछा यकायक आना हुआ कोई ज़रूरी काम है क्या? मैंने कहा, जी, चलिए इंदिरानगर चलना है। वहॉं पहुँचकर उन्होंने पूछा, अब कहॉं ? मैंने कहा, वाल्मीकि बस्ती में। वे मेरे जवाब से थोड़े चौंके। बस्ती में पहुँचते हीरालाल मिले। गले से लग गए।आतिथ्य की उत्तेजना में उन्हें समझ नहीं पड़ रहा था कि मुझे क्या खिला दें? क्या पिला दें? वे कुछ पूजा पाठ में लगे थे।
शायद कथा सुन रहे थे। उन्हें पूजा पाठ में देख मैं कुछ अचम्भित हुआ। हीरालाल भॉंप गए। कहा हम भी कथा सुनते हैं गुरू जी।फिर हीरालाल किसी वैदिक पंडित की तरह मुझे प्रवचन देने लगे।
“आप तो जानते हैं हमारी परम्परा में निगम, आगम और कथा परम्परा है। निगम में वेद उपनिषद आरण्यक और ब्राह्मण ग्रन्थ आते हैं। आगम में बौद्ध, जैन और तंत्र ग्रन्थ हैं और कथा परम्परा में रामायण, महाभारत और पुराण। गुरू जी कथा परम्परा के तीनों आचार्य दलित थे।” हीरालाल के कथन में गर्व का भाव था।” वाल्मीकि, वेद व्यास, और सूत जी इन तीन दलित महर्षियों ने ही हमारे समाज को रामकथा, कृष्ण कथा और पुराण कथा दी। एक त्रेता में दूसरे द्वापर में और तीसरे कलियुग में थे।
इन तीन दलित महर्षियों पर ही हमारी संस्कृति टिकी है।” पहली बार हीरालाल की विद्वता के आगे मैं नतमस्तक था। शादी दिन में ही थी। भोजन के बाद हम लौट रहे थे। हीरालाल के स्नेह और ज्ञान में आकण्ठमग्न होकर।
पर हीरालाल का ये स्नेह मन में कई तरह के सवालों को भी जन्म दे रहा था।आख़िर हम किस समाज में जी रहे हैं जहॉं इस वर्चुअल युग में भी हमारी जातीय पहचान दो जगह अब भी बची है।पहला मंदिर और दूसरा शौचालय। हर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण ही होगा और हर शौचालय की साफ-सफाई का काम वाल्मीकि ही करेगा।दोनों जगह जाति की जो घेराबंदी है, उसे तो टूटना चाहिए। समतामूलक समाज के लिए यह जरूरी है। ज्ञान के स्तर पर हीरालाल मुझसे बराबरी पर थे।तो सामाजिक लिहाज़ से क्यों न हों ।
आप ज़रा सोचिए, हमारे देश में 9 करोड़ से अधिक वाल्मीकि हैं। लेकिन हर शहर, संस्थान और गांव में सफाई कर्मचारी के नाते वाल्मीकि ही क्यों मिलते हैं? दुनिया में इससे बढ़कर अभिशाप किसी और जाति को मिला है क्या? कि जो जन्मते ही सफाई कर्मचारी बन जायें? पाकिस्तान की सेना ने पिछले दिनों एक विज्ञापन छापा था कि उन्हें सेना में सफाई कर्मचारी के लिए हिन्दू वाल्मीकि जाति के लोग चाहिये। पता नहीं उस वक्त हिन्दू धर्म की बात करने वाले लोगों का खून खौला या नहीं?
समय बदला है पर इस समुदाय की स्थिति नहीं बदली। मुगलों के आने से पहले ये भंगी कहे जाते थे। मुग़लों ने इन्हे मेहतर बना दिया, पर बेहतर कुछ नहीं हुआ। मुक्ति बोध लिख गए हैं-
“जो है उससे बेहतर चाहिए
पूरी दुनिया साफ करने के लिए,
मेहतर चाहिए।”
मगर अफसोस कि पूरी दुनिया की सफाई का हक और श्रेय रखने वाली इस कौम का भला नही हुआ। न अंग्रेजों के समय में,न आजादी के बाद ही। आजादी आने के बाद भी यह जाति मैला ढोने से आजाद नहीं हो सकी है। बड़ा सवाल है कि इस दौर में जब जूता-चप्पल, लोहा-लकड़ी और सोने-चांदी की दूकानें जातीय पहचान खो रही हैं तो फिर सिर्फ मेहतर या सफाई वाले ही जातीय पहचान क्यों बनाए हुए हैं?
आखिर क्यों इस पर कोई विमर्श नही होता? जब-जब मुझे हीरालाल और सलाम चाचा की याद आती है, ये सवाल अचानक ही मेरे जे़हन को मथने लगता है। समय तमाम प्रश्नों के हल खुद करता है।उम्मीद है शायद एक रोज़ समय के रोस्टर में इस सवाल के हल की भी बारी आए।