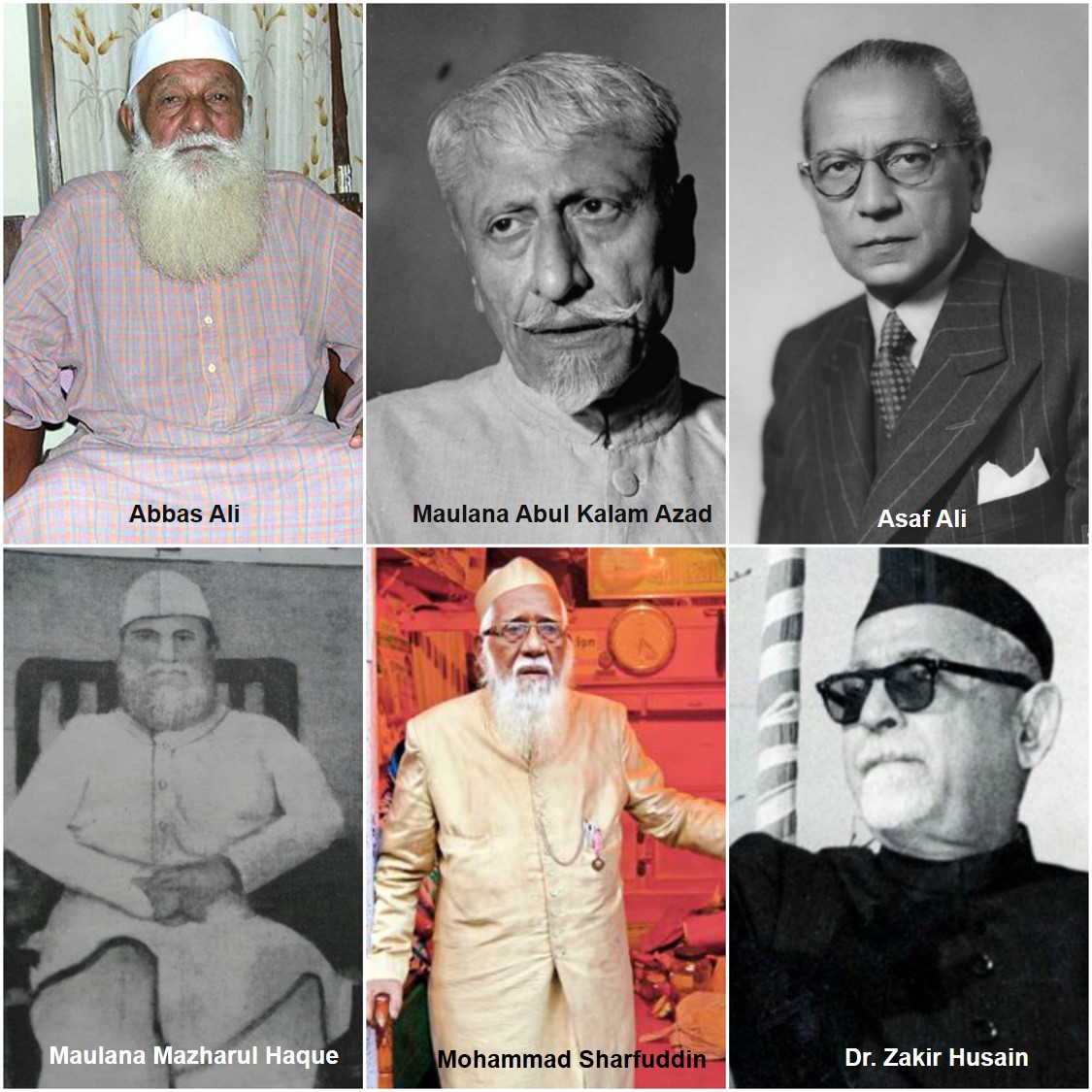सोशल मीडिया ने एक युगांतकारी काम यह किया है कि जो जटिल विषय पहले विद्वानों के बीच बहसबाजी के मौजूँ थे उन विषयों पर अब हर कोई बहस करता है या कर सकता है। बुद्धिजीवियों ने अपनी बहसों के लिए आम अखबारों-पत्रिकाओं से अलग अकादमिक रिसाले बना रखे हैं।
आला दर्जे के रिसाले वो माने जाते हैं जिसमें कोई नया पर्चा तभी छपता है जब उसे विषय का पुराना अध्येता पढ़कर सहमति दे दे कि इन्होंने जो तथ्य और हवाले दिये हैं वो सही हैं। मसलन, कोई तुलसीदास पर पर्चा लिख रहा है और दावा कर रहा है कि तुलसी न ऐसा लिखा है तो उसे हूबहू छापना उचित नहीं। किसी को यह जाँचना चाहिए कि सचमुच तुलसी ने वैसा लिखा भी है या नहीं। इसी देश में अदालत तक में तुलसी के नाम पर नकली किताब सबूत के तौर पर पेश की गयी है।
यही वजह है कि ज्यादातर अकादमिक विद्वान सोशलमीडिया से चिढ़ते हैं। यहाँ पाँचवीं पास, दसवीं पास, रेडियो जॉकी या कम्प्यूटर इंजीनियर भी तुलसीदास या दुर्खाइम या हाइजनबर्ग पर चलने वाली बहस में कूद पड़ता है। ये लोग नहीं मानते कि किसी भी विषय के अध्ययन-प्रशिक्षण में वक्त लगता है। आज विकिपीडिया आपको किसी विषय पर बहस के लिए तैयार कर सकता है। अखबारों, पत्रिकाओं, अकादमिक रिसालों में तो सम्पादक के रूप में एक रेफरी होता है लेकिन सोशलमीडिया पर कोई रेफरी नहीं है। यहाँ आदमी सीधे सिर फुटव्वल करने के लिए आजाद है।
कभी-कभी इन हालात से मन झुंझला जाता है। कई बार कुछ लोगों पर तेज गुस्सा भी आ जाता है। कई बार बहुतों को गुस्से में डांटा भी। कई बार जानबूझकर ऐसी बातें कहीं जो पता थीं कि सामने वाले को तिलमिला देंगी। लेकिन पारा सामान्य होने के बाद यही लगता है समझदारी और परिपक्वता दिखाने का दायित्व तो सामने वाले से ज्यादा हम लोगों के सिर पर है।
हम लोग यानी जो देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों से पढ़े। जिनको सबसे अच्छी टीचर और किताबें मिलीं। जहीन संगी-साथी मिले जो हर विषय पर रोशनख्याली के साथ बहस कर सकें। अगर ऐसे लोग गाहे-बगाहे या स्थायी तौर पर ट्रॉल में बदल रहे हैं तो फिर हम किस मुँह से उन लोगों को नसीहत करें जिनको ढंग से शिक्षा भी नहीं मिली।
आज ही मैं इस्लामिक इतिहास पर एक लेक्चर देख रहा था जिसमें वक्ता ने जाहिल शब्द पर चर्चा की। आम तौर पर जाहिल का मतलब अशिक्षित से लगाया जाता है। कुछ दीनी किस्म के मुसलमान मानते हैं कि जिसके पास इस्लाम का इल्म नहीं है वो जाहिल है। लेकिन हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल के पीएचडी स्टूडेंट जवाद हाशमी के अनुसार जाहिल जहल से बना है और उसका एक शुरुआती अर्थ यह था कि जो बहुत आसानी से उत्तेजित या क्रोधित हो जाये। यह भी बताया गया कि जाहिल का विलोम था हिल्म (संयमित और मर्यादित) और इसलिए मोहम्मद को हलीम कहा गया यानी जो हिल्म के ऊँचे मेयार पर हो। इस तीसरे लिहाज से तो मैं भी जाहिल साबित होता हूँ।
अशिक्षित या अर्धशिक्षित लोगों की बात छोड़ देते हैं। आज शिक्षित जन भी आलोचना करने और अपमानित करने के बीच फर्क भूल चुके हैं। ऐसा लगने लगा है जैसे हम सब एक दूसरे को अपमानित करने के राष्ट्रीय अभियान पर हैं। सच कहूँ तो मैंने अपने अन्दर भी यह प्रवृत्ति कई बार चिह्नित की है। कुछ समय पहले अन्यान्य कारणों से करीब सात साल पुरानी अपनी एक पोस्ट पर पहुँच गया। वहाँ एक युवा हिन्दी लेखक से किसी मुद्दे पर तीखी बहस मौजूद थी। मैं यह देखकर दंग रह गया कि उस बहस में मेरा टोन बहुत रूड था। नीचा दिखाने या बेवकूफ समझकर बहस करने वाली शैली में कोई सार्थक संवाद सम्भव नहीं है। आज भी यह गलती मुझसे जब नहीं तब हो जाती है। मुझे लगता है कि यह सामंती औपनिवेशिक समाज का लक्षण है। जिसमें सभी किसी विदेशी ताकत के गुलाम हों जो उन्हें हीन समझकर बरताव करती है तो वो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाकर उस हीनभावना की भरपाई करते हैं।
आलोचना और अपमान के बीच का यह अन्तर समझना आज बहुत जरूरी है। आलोचना की प्रकृति शीतल होती है, अपमान की गरम। नामवर सिंह का जुमला ‘मतभेद है मनभेद नहीं’ लोकप्रिय है। इसका इस्तेमाल करूँ तो कहना चाहूँगा कि आलोचना मतभेद को व्यक्त करती है, अपमान मनभेद को। जिससे आपका इमोशनल ब्रेक-अप हो जाये फिर उसकी कोई बात कहाँ सुहाती है!
क्या हम बौद्धिक इसलिए ही बने हैं कि किसी अन्य समुदाय, धर्म, जाति या देश को अपमानित कर सकें। मूल्यों की पैरोकारी और उनपर बहस लोकतंत्र का प्राण है लेकिन इस कवायद में अमानवीयता और असभ्यता के स्तर पर पहुँच जाने का अर्थ है कि मूल उद्देश्य पीछे छूट चुका है। अतः आपसे अनुरोध है कि एक बार जरूर सोचें कि आपके लेखन की प्रेरणा आलोचना है या अपमान।