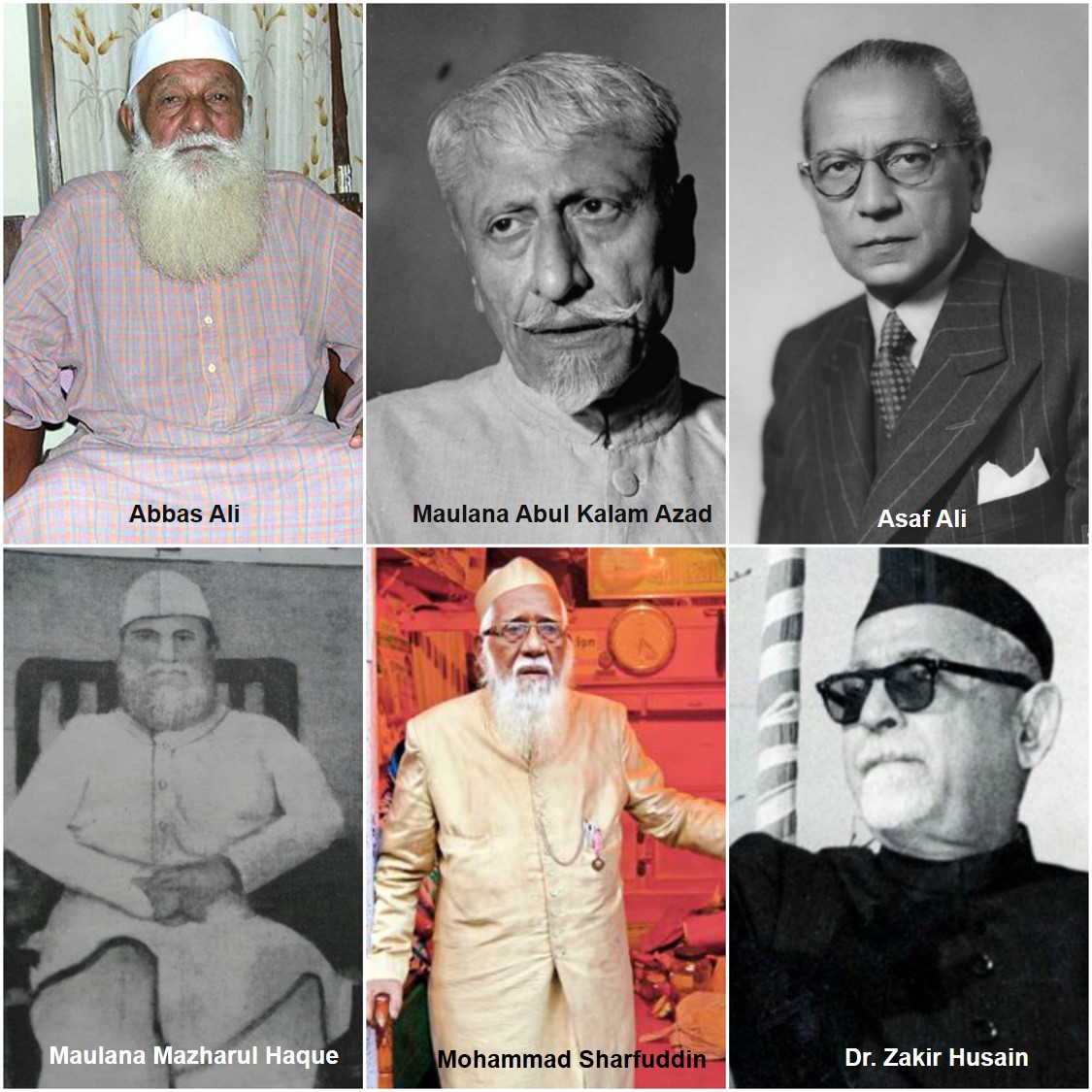क्या मार्क्सवाद का अंत हो चुका है? कार्ल मार्क्स के जन्म के दो सौवें साल में बहुत निश्चयात्मक ढंग से इसके प्रमाण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उस सोवियत रूस का अस्तित्व ही नहीं बचा जिसने मार्क्सवाद का पहला प्रयोग किया था। पूर्वी यूरोप के वे देश धूल में मिल गए- कुछ तो गायब हो गए- जहां मार्क्सवादी शासन व्यवस्था थी। पूर्वी जर्मनी, युगोस्लााविया, चेकोस्कोवाकिया जैसे देश नक्शे में नहीं मिलते, जबकि हंगरी-पोलैंड बिल्कुल बदले हुए है। कभी अमेरिका को धूल चटाने वाला वियतनाम अब भूमंडलीकृत दुनिया का हिस्सा है। एशिया में चीन का मार्क्सवाद अब बाज़ारवाद से गलबंहियां करके चल रहा है। भारत में मार्क्सवाद के गढ़ एक-एक कर टूट रहे हैं। बंगाल हाथ से निकल चुका है, केरल में वाम संघर्ष तीखा है और अकेला त्रिपुरा है जिसे सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी बीजेपी के लिए वाटरलू घोषित करने का उत्साह दिखा रहे हैं। इसके समानांतर वामपंथ या मार्क्सवाद की वैचारिकी अपराध मिश्रित नक्सली हिंसा की चपेट में है और ऐसा लाल गलियारा बना रही है जो सत्ता के लिए चुनौती भले पैदा करता है, उसकी हिंसा को एक वजह मुहैया कराता है।
बौद्धिक हलकों में इन दिनों मार्क्सवाद का मज़ाक उड़ाने का मौसम है। मार्क्सवादी राजनीति के अपने अंतर्विरोध इसकी वैध वजहें भी मुहैया कराते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्टालिन से लेकर चाउशेस्कू तक- मार्क्सवाद के नाम पर अपराध और लूट की ऐसी भीषण परियोजनाएं चलाई गई हैं जिनका ज़िक्र किसी वास्तविक मार्क्सवादी को शर्मिंदा करता है। बाज़ार की विराट आधुनिक परियोजना में मार्क्सवादी वैचारिकी बीते ज़माने और बीती दुनिया की चीज़ है। इसके अलावा इन दिनों सत्ता द्वारा वे लोग पुरस्कृत किए जा रहे हैं जो मार्क्सवाद ध्वंस के घोषित यज्ञ में लगे हुए हैं। मार्क्सवाद विरोध इतना आसान, सुविधाजनक और पुरस्कृति की संभावना से भरा पहले कभी नहीं रहा।
लेकिन मार्क्स और मार्क्सवाद के तथाकथित शव के चारों ओर चल रहे पूंजीवादी प्रेतों के इस उद्धत नृत्य के पार अगर देखें तो कुछ और सच्चाइयां दिखाई पड़ती हैं। सिर्फ सत्ता केंद्रित विमर्श में लीन जो लोग मार्क्स की श्रद्धांजलि लिखते नहीं अघा रहे हैं, उन्हें बस यह याद दिलाने की ज़रूरत है कि मार्क्सवाद सत्ता में रहे या नहीं, वह राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है। इस मार्क्सवाद की अवहेलना कर कोई भी राजनैतिक एजेंडा परवान नहीं चढ़ सकता।
दरअसल मार्क्स ही नहीं, उन्नीसवीं सदी के कुल जमा तीन ऐसे विचारक हुए जिन्होंने दुनिया के सोचने का ढंग हमेशा-हमेशा के लिए बदल दिया। कार्ल मार्क्स ने शोषण और विषमता की बात की, याद दिलाया कि जो उत्पादन करता है, वह सर्वहारा बना हुआ है, पूंजी का एक मनुष्यविरोधी स्वभाव है और दुनिया के मजदूरों को एक होना होगा, किसानों को उत्पादन में अपनी मिल्कियत हासिल करनी होगी। मार्क्सवाद के मुक़ाबले के लिए निरंकुश पूंजीवाद ने अपना चोला बदला, मार्क्स के ही दबाव में कल्याणकारी राज्य की अवधारयणा विकसित हुई और वह पूरा राजनीतिक मुहावरा हमेशा-हमेशा के लिए बदल गया जिसके आधार पर सत्ताएं हासिल की जाती हैं या गवाईं जाती हैं।
मार्क्स 5 मई 1818 को पैदा हुआ था, सिगमंड फ्रायड 6 मई को- बेशक, मार्क्स की पैदाइश के 38 बरस बाद। लेकिन फ्रायड वह दूसरा चिंतक है जिसने आने वाली सदियों के चिंतन पर सबसे गहरा असर डाला। फ्रायड ने बताया कि बाहर की जो दुनिया है, उसका हमारे अवचेतन से बहुत गहरा वास्ता है। इस दुनिया की गुत्थी को ठीक से समझने के लिए ज़रूरी है कि मन के भीतर झांकें।
मार्क्स और फ्रायड से कई बरस पहले हुआ चार्ल्स डारविन, जिसने बताया कि न मनुष्य ब्रह्मा के मुख से निकला है न हव्वा किसी आदम की पसली से निकली है। सब सरल से जटिल होते संसार का हिस्सा हैं और इंसान का सबसे क़रीबी पुुरखा बंदर है। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत ने भी दुुनिया का चिंतन बदलने में अहम भूमिका अदा की।
मार्क्सवाद पर लौटें। यह सच है कि डार्विन या फ्रायड की तरह ही मार्क्स के कई आकलनों की सीमाएं बाद में खुली हैं, उनके अंतर्विरोध भी सामने आए हैं, उनके राजनीतिक अनुयायियों की बर्बरता सबको शर्मिंदा करती रही है, मार्क्सवाद के नाम पर की जाने वाली चूकें उसे उपहासास्पद बनाती रही हैं, लेकिन इससे बड़ा यह सच है कि मार्क्स ने जाने-अनजाने दुनिया का राजनीतिक एजेंडा बदल दिया है। औद्योगिक क्रांति के बाद मजदूरों के एक होने का मार्क्स का आहवान न होता तो शायद पूंजी अचानक इतनी उदार और मानवीय न हो उठती। यह सच है कि मार्क्सवाद के दबाव में पूंजीवाद ने ख़ुद को कुछ मानवीय बनाने की कोशिश की। मज़दूरी के घंटे, रिटायरमेंट की योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा के प्रश्न- यह सब कामकाज की दुनिया में इसी के बाद आए। यह अनायास नहीं है कि मार्क्सवाद के तथाकथित पतन के बाद पूंजी अचानक निरंकुश दिखने लगी है, मजदूरों की दुनिया कहीं ज़्यादा निरीह और असुरक्षित नज़र आ रही है।
जहां तक भारत का सवाल है, मार्क्सवाद की कई विडंबनाएं उजागर हैं। दो दशक से ज़्यादा समय तक बंगाल पर राज करने वाला वाम मोर्चा इस तरह पराजित है कि उसकी तत्काल वापसी के आसार नहीं दिख रहे। लेकिन दिलचस्प यह है कि वाम मोर्चा तब पराजित हुआ, जब उसने वाम मुद्दों का साथ छोड़़ा- और ममती बनर्जी इसलिए जीतीं कि उन्होंने वाम का विरोध करते हुए भी मुद्दे वही उठाए जो वाम राजनीति में केंद्रीय हुआ करते हैं। इस राजनीतिक पराजय के अतिरिक्त वाम विचारधारा इन दिनों अपनी माओवादी धारा की वजह से लोकतांत्रिक विश्वासों वाले मार्क्सवादियों के लिए दुविधा का विषय बनी हुई है। यह स्पष्ट है कि ऐसे हिंसक और मूलतः अलोकतांत्रिक आंदोलन अपनी नैतिक आभा भी खो चुके हैं और रणनीतिक तौर पर भी विफल होने को अभिशप्त हैं। उनकी वजह से राज्य की हिंसा को भी वैधता मिली है और बहुत सारे आम लोगों को इसका शिकार होना प़ड़ा है। इसके अलावा आंदोलन के बंद चरित्र की वजह से इसमेंं बड़़ी तादाद में अपराधी तत्वों की भी घुसपैठ हुई है जिनके लिए माओवाद खाने-कमाने का मामला बना हुआ है। लेकिन इन सबके बावजूद ज़्यादा बड़ा यह सच है कि यह माओवादी गलियारा इसलिए बड़ा हो रहा है कि मजदूरों, किसानों, आदिवासियों और दलितों की उपेक्षा बड़ी हो रही है, उनका असंतोष बड़ा हो रहा है और वहां के संसाधनों की लूट बड़़ी हो रही है। पूंजी के लगभग एकाधिकारवादी होते निरंकुश होते चरित्र और लोकतांत्रिक संस्थानों पर उसके अभेद्य होते क़ब्ज़े ने हाशिए पर पड़े समुदायों में जो मायूसी पैदा की है, वह तरह-तरह से फूट रही है, इससे बाहर निकलने के रास्ते खोज रही है और एक रास्ता वह माओवाद सुझाता है जो अपने लिए मार्क्सवाद की वैचारिकी से खुराक हासिल करता है।
सवाल है, क्या मार्क्सवाद सिर्फ़ वैचारिक औज़ार बना रहेगा या सत्ता में उसकी उस तरह ठोस वापसी होगी जैसी बीसवीं सदी के लंबे दौर में रही? इसका कोई निश्चित जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन सोवियत रूस के आख़िरी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाच्यौफ़ ने अपनी किताब ‘पेरेस्त्रोइका’ में एक दिलचस्प बात लिखी है। गोर्बाच्यौफ़ ने याद दिलाया कि दुनिया की कोई क्रांति एक दौर में पूरी नहीं हुई है। वे बताते हैं कि 1789 में हुई फ्रांसिसी क्रांति कई तरह के बदलावों से गुज़रती हुई अंततः पांचवें गणतंत्र तक जाकर पूरी हुई। उसी दौर की अमेरिकी क्रांति ने अमेरिकी गृह युद्ध देखा, लिंकन की हत्या देखी और धीरे-धीरे सुस्थिर हुई। ब्रिटेन में हुई 1688 की गौरवशाली क्रांति ने कई दौर देखे, 1832 के संसदीय सुधार देखे और फिर एक मो़ड तक पहुंची। गोर्बााच्यौफ का कहना था कि रूसी क्रांति भी एक दौर में पूरी नहीं होगी। उसमें भी अलग-अलग दौर आएंगे।
गोर्बाच्यौफ़ की यह भविष्यवाणी अपनी जगह है, मगर यह सच है कि सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवाद के पतन के बाद दुनिया कुछ बेहतर हुई हो, इसके सबूत नहीं मिलते। उल्टे, पश्चिम एशिया में बीते दो दशकों में जो कुछ हुआ है, उसने सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, एक ऐसा सांस्कृतिक संकट भी पैदा कर दिया है जिसके साये सारी दुनिया पर हैं। तालिबान, अल क़ायदा और आईएस- तीनों अमेरिकी एकध्रुवीयता की महत्वाकांक्षा, उसके अहंकार और छल की पैदाइश हैं। दुनिया कई तरह के धार्मिक और प्रादेशिक टकरावों की गिरफ़्त में है। संस्कृतियों और समुदायों में आपसी नफ़रत और कट्टरता बढ़ी है। आर्थिक मोर्चे पर भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। अर्थव्यवस्थाएं बड़े और खगोलीय उद्यमों की मुट्ठी में हैं और अक्सर हिचकोले खाती नज़र आ रही हैं। दुनिया भर में बेरोज़गारी इस तरह बढ़ी है कि अलग-अलग देश दूसरे नागरिकों के लिए अपने दरवाज़े बंद कर रहे हैं। यही नहीं, यह पूंजीवादी तंत्र धीरे-धीरे वास्तविक लोकतंत्र का अपहरण कर जनादेश को बंधक बनाता भी नज़र आ रहा है।
इस लिहाज से देखें तो मार्क्सवाद का यूटोपिया चाहे जितना ब़डा हो, दुनिया को मार्क्सवाद की ज़रूरत उतनी ही बड़ी है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि इन सारे संकटों के समाधान मार्क्सवाद के भीतर हैं, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि पूंजीवाद की यह अनिश्चितता जिन विकल्पों की ओर ध्यान खींचती है, उनमें मार्क्सवाद सबसे बड़ा विकल्प है। समानता और स्वतंत्रता की लड़ाई के जो बहुत सारे चेहरे हैं, उनका वास्ता कहीं न कहीं मार्क्स के सिद्धांतों से है। उनकी मौजूदा विफलता उनका स्थायी अंत नहीं है। दुनिया भर में पूंजी की विराट परियोजनाओं से लोहा ले रहे जो छोटे-छोटे अभियान हैं, सांप्रदायिकता, उग्र राष्ट्रवाद और नस्लवाद के ख़िलाफ़ जो छापामार लड़ाइयां हैं, बराबरी के हक़ में चलाए जा रहे जो आंदोलन हैं, वे सब इस बात की तस्दीक करते हैं कि मार्क्सवाद ज़िंदा है और उसे यह भरोसा है कि एक दिन दुनिया बेहतर और बराबर होगी।
प्रिय दर्शन