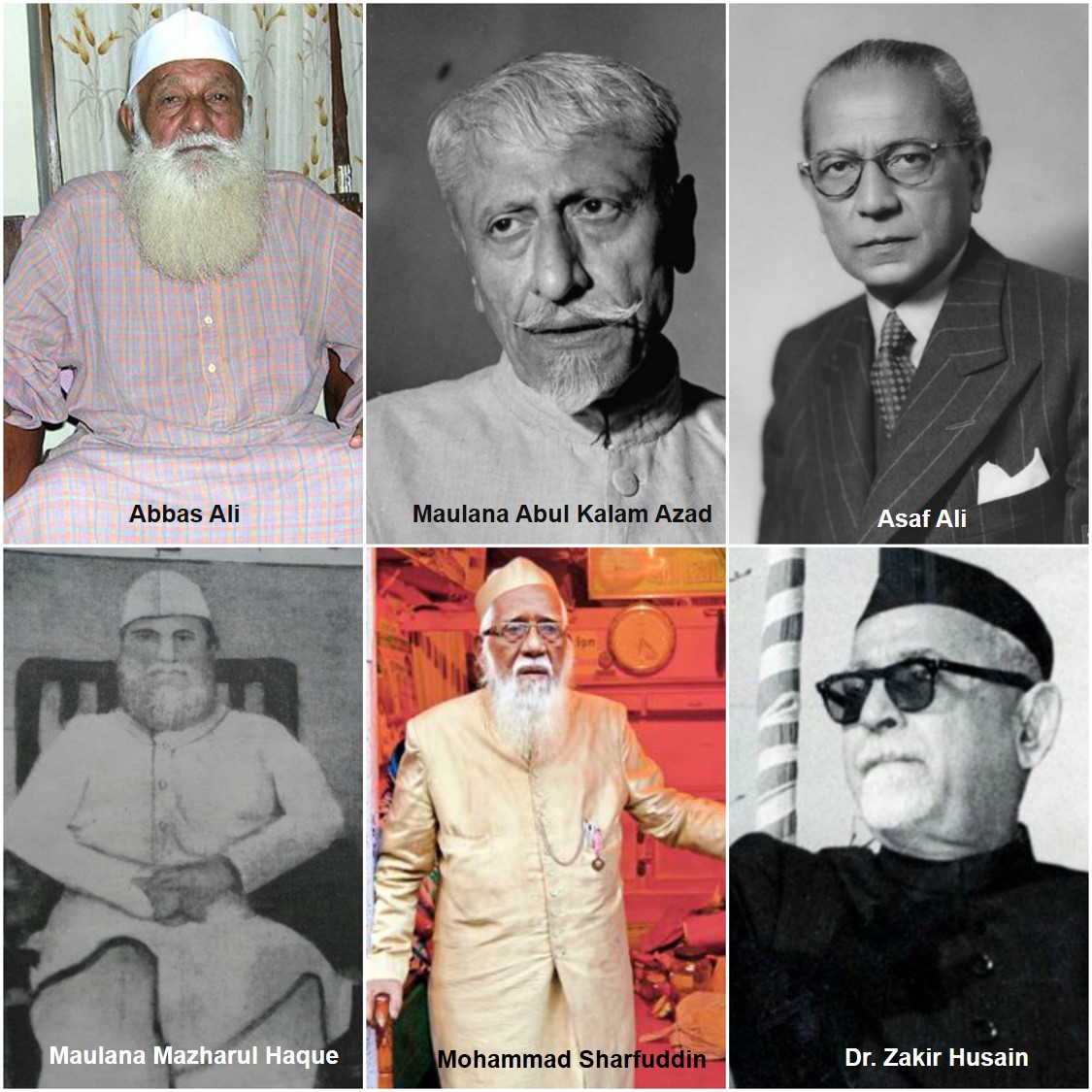फ़िल्म निर्देशक, बुद्धदेव दासगुप्ता
हिंदी सिनेमा का दर्शक जब बुद्धदेव दासगुप्ता को याद करता है तो फिल्म ‘बाघ बहादुर’ स्मृतियों कौंध जाती है। यह एक ऐसे इंसान के सामाजिक और आंतरिक अंतर्द्वंद्व की कहानी थी जिसने बाघ को अपने भीतर आत्मसात किया था।
बुद्धदेव का सिनेमा यथार्थवादी होता था मगर वह यथार्थ के फंतासी में बदलने की सीमा को बस जैसे छूकर लौट आता था। ‘बाघ बहादुर’, ‘तहेदार कथा’, ‘चराचर’, ‘लाल दारजा’ उनकी इसी शैली में बनाई गई यादगार फिल्में हैं। शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि बुद्धदेव दासगुप्ता फिल्म निर्देशक होने के साथ-साथ एक कवि भी थे।
कविता को उस तरह नहीं समझा जा सकता जैसे हम कथा साहित्य को समझते हैं। कविता हमेशा अपने पाठक या श्रोता से एक विशेष संवेदना और समझ की मांग करती है। कविता न समझ में आने पर बहुत दुरूह और समझ आए तो हृदयग्राही हो जाती है। यथार्थ की सीमा का अतिक्रमण करती हुई अपनी फिल्मों में वे अक्सर समाज में हाशिये पर टिके हुए किरदारों को फिल्म के केंद्र में ले आते थे।
अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, “मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो भौतिकवादी नहीं हैं, जो भावुक और संवेदनशील हैं, जो बात करते-करते खो जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो बहुत अधिक व्यावहारिक होते हैं, जो चीजों को जल्दी समझ लेते हैं। मेरी फिल्मों के चित्र और पात्र बेहद आंतरिक और व्यक्तिगत हैं।”
बुद्धदेव को आधुनिक सभ्यता के आलोचक के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि उन्होंने ‘अंधी गली’ जैसी राजनीतिक फिल्म भी बनाई है मगर ज्यादातर फिल्मों में सांस्कृतिक विस्थापन की ही पड़ताल है। ‘बाघ बहादुर’ फिल्म इसे बड़ी सूक्ष्मता से दर्शाती है कि कैसे कोई समाज विकास के नाम पर अपनी सामूहिकता की संस्कृति को नष्ट करता है और वह एक पारंपरिक ग्रामीण कलाकार के लिए उसके अस्तित्व का संकट बन जाता है।
घुनुराम एक मामूली मजदूर है मगर एक परंपरा है, जिसमें वह बाघ का रूप धारण करते नृत्य करता है और यही अपने समाज में उसकी आइडेंटिटी है। बाघ का यह रूप एक मामूली मजदूर बने रहने की बजाय उसे एक कलाकार के रूप में सामने आने का मौका देता है, जिससे गांव के सभी लोग प्यार करते हैं। यही पहचान उसे एक पूर्णता का एहसास करती है। मगर पारंपरिक और आधुनिक जीवन शैली के बीच संघर्ष धीरे धीरे उसे हाशिये पर धकेल देता है।
इस फिल्म का बुद्धदेव की स्मृतियों से गहरा रिश्ता है। बचपन में उन्होंने कुछ साल खड़गपुर में बिताए थे। जहां की संस्कृति पूरी तरह से बंगाली नहीं थी। आबादी का एक हिस्सा तेलंगी समुदाय से आता था। ये लोग आंध्र प्रदेश से विस्थापित होकर आए थे। वहीं पर बुद्धदेव ने बाघ नर्तकों को देखा। जो लोक कलाकार थे और बाघ की वेशभूषा बनाकर गाते और नृत्य करते थे।
आधुनिक सभ्यता के आलोचक की यह दृष्टि शायद बुद्धदेव ने अपने आरंभिक जीवन और बचपन से ही प्राप्त की थी। शहर उन्हें हमेशा से परेशान करता था। बुद्धदेव के पिता भारतीय रेलवे में कार्यरत डॉक्टर थे। उनका बचपन ज्यादातर छोटे शहरों और कसबों में रेलवे के आवास में बीता।
वे अपने एक साक्षात्कार में बचपन के दिनों को याद करते हुए कहते हैं, “मुझे खड़गपुर में रहते हुए घास में लाल कीड़ों के साथ खेलना याद है। मेरे बचपन ने मुझे अनगिनत छवियां दीं जो मेरी फिल्मों में लौटती हैं।” गौर करें तो उनकी फिल्मों के नायक अक्सर प्रकृति और बचपन में लौटने की ललक लिए नजर आते हैं। वे कविताएं भी लिखते थे। ऐसा लगता है कि एक समय के बाद वे अपनी सिनेमाई भाषा को कविता के करीब ले जाना चाहते थे।
उनकी इन सैल्यूलाइड पर लिखी कविताओं के केंद्र में अक्सर प्रकृति नजर आती है। इन फिल्मों में प्रकृति सिर्फ एक परिवेश नहीं है, बल्कि एक चरित्र की तरह मौजूद है। इसीलिए दासगुप्ता की फिल्मों में एक किस्म का अमूर्तन सा महसूस होता है मगर वह कोरी दार्शनिकता नहीं है बल्कि उसे खोला जा सकता है, उन प्रतीकों और बिंबों को डिकोड किया जा सकता है।
उनकी आरंभिक फिल्मों में नक्सलबाड़ी आंदोलन के प्रति मोहभंग दिखता है। जब नक्सलबाड़ी विद्रोह हुआ तब बुद्धदेव एक छात्र थे। समय बीतने के साथ उन्हें यह महसूस हुआ कि नक्सलवाद उन्हीं लोगों को खोता जा रहा है जिनके बीच से उसका आरंभ हुआ था। आंदोलन के हिंसक होने के साथ ही यह भी लगा कि वास्तव में कुछ बदल नहीं रहा है।
हिंसा को हमारे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में इतने करीब से महसूस करने की वजह से ही उनकी फिल्मों में प्रकृति के बाद जिस दूसरे तत्व का सबसे सूक्ष्म निरूपण है, वह हिंसा ही है। वे कहते थे, “हम डर को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं। हम जागते हैं, भय भी जाग जाता है, सारा दिन हमारा पीछा करता है, और फिर हमारे साथ सोने के लिए लौट आता है।”
नक्सली आंदोलन और इसकी विफलता के प्रति उनका यह विमर्श दूरत्व (1978), गृहजुद्धा (1982) और अंधी गली (1984) जैसी फिल्मों में देखा जा सकता है। अस्सी के दशक में आई उनकी फिल्म ‘गृहजुद्धा’ पर मृणाल सेन की शैली का असर दिखता है। शायद इसकी एक वजह यह हो सकती है कि मृणाल सेन ने नक्सली आंदोलन पर भी कुछ बहुत ही अहम फिल्में बनाई हैं।
हालांकि उस वक्त के युवा निर्देशक बुद्धदेव ने नक्सली आंदोलन के बारे में बिल्कुल अलग तरीके से बात की। निरुपमा (ममता शंकर) नक्सल आंदोलन में अपने भाई को खो देती है, फिल्म उसके नजरिए से बंगालियों की एक पूरी पीढ़ी की चेतना को आकार देती है। इस तरह दासगुप्ता अपनी आरंभिक फिल्मों में कोलकाता और उसके आसपास के परिवेश में रची-बसी कहानियां कह रहे थे, जो उनके वरिष्ठ मृणाल सेन और सत्यजीत रे के सामाजिक यथार्थवाद के काफी करीब थीं।
सन् 1992 में बनी फिल्म ‘तहदेर कथा’ की कहानी एक स्वतंत्रता सेनानी सिबनाथ (मिथुन चक्रवर्ती) के इर्द-गिर्द घूमती है। जिसे एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के लिए 11 साल की कैद के बाद रिहा किया गया है। फिल्म के अलग अलग प्रसंगों से गुजरते हुए बुद्धदेव आपको अपने नायक के दिमाग के सबसे गहरे, अंधेरे कोनों में ले जाते हैं।
धीरे-धीरे उनकी फिल्मों में काव्यात्मकता बढ़ती नजर आती है। उनकी सर्वाधिक काव्यात्मक फिल्मों में से एक ‘चराचर’ में बुद्धदेव दासगुप्ता एक बार फिर हाशिये पर जीने वाले किरदार लाखा से मिलाते हैं, जो एक पक्षी पकड़ने वाला है, और जिसे अपने जाल में फंसे जीवों के प्रति बहुत सहानुभूति है। दासगुप्ता इस फिल्म को अपने बहुत करीब पाते हैं।
द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में वे कहते हैं, “तुम्हें पता है, कभी-कभी मैं खुद को अपनी फिल्म ‘चराचर’ के केंद्रीय चरित्र लाखा के रूप में देखता हूं। मुझमें कुछ ऐसा है जो मेरे द्वारा बनाए गए हर किरदार में समाहित हो जाता है। जब मैं फिल्में बनाता हूं तो अपने बचपन में वापस जाता हूं और अपने अतीत से तस्वीरें उधार लेता हूं। आप उन्हें आत्मकथात्मक नहीं कह सकते लेकिन मैं इनमें से प्रत्येक फिल्म मैं मौजूद हूँ।”
इसी तरह से ‘उत्तरा’ को उनकी सर्वाधिक विचारोत्तेजक फिल्म माना जा सकता है। इसमें बहुत से प्रतीकात्मक तत्व हैं, जिन्हें फिल्म की समीक्षा या उसे पढ़ने के दौरान डिकोड किया जाना चाहिए। एक स्तर पर यह फिल्म कट्टरपंथ को अपना विषय बनाती है मगर यह काफी आगे जाते हुए उत्पीड़ितों की यौन मुक्ति की बात करती है।
प्रकृति का विध्वंस उन्हें चिंतित करता था। बचपन में पिता के साथ पहाड़ियों पर देखी जंगल की आग उन्हें हमेशा याद रही। अपनी फिल्मों के जरिए वे बार-बार अपने बचपन की स्मृतियों और कहानियों की तरफ लौटते थे। कालपुरुष’ पिता के साथ नायक के संबंधों को एक अलग स्तर पर ले जाती है। अपने एक साक्षात्कार में दासगुप्ता बताते हैं, इस फिल्म को देखने के बाद कई लोगों ने मुझे फोन किया। वे रोए और अपने पिता को याद किया।
वे आगे कहते हैं, “मेरी कोई भी फिल्म आत्मकथात्मक नहीं है। लेकिन मेरे काम में आत्मकथात्मक तत्व स्वाभाविक रूप से लौटते रहते हैं। कालपुरुष एक ऐसी ही फिल्म थी। मैंने इसकी विषय वस्तु को महसूस किया, समझा, सूंघा। जब मैं छोटा था तब मेरे पिता बहुत व्यस्त थे। वह हमें समय नहीं दे सके। लेकिन मैं उन्हें समझने में कभी असफल नहीं हुआ। मैं समझ गया कि वह अपने बेटे के साथ किस तरह का रिश्ता रखना चाहते होंगे।”
जब हम बुद्धदेव दासगुप्ता के सिनेमा पर बात करते हैं तो निर्विवाद रूप से बंगाल के ही एक और महान निर्देशक ऋत्विक घटक की याद आना स्वाभाविक है। भारत में सिनेमा पश्चिम से आया था, लिहाजा यह स्वाभाविक था कि हमारे सबसे बेहतरीन निर्देशकों पर भी पश्चिम का असर देखने को मिलता है। अपनी फिल्मों के माध्यम से भारतीय सिनेमा को दुनिया में पहचान दिलाने वाले सत्यजीत रे, बिमल राय, गुरुदत्त जैसे निर्देशकों ने भी स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि उन पर पश्चिमी निर्देशकों और फिल्मों का असर रहा है।
आश्चर्यजनक रूप से ऋत्विक घटक और उसके बाद बुद्धदेव ऐसे किसी भी असर से मुक्त नजर आते हैं। अपनी शैली और सिने छवियों की इस मौलिकता के बारे में बुद्धदेव कहते हैं, “मैं संगीत, चित्रकला और कविता का बहुत ऋणी हूं। मेरी मां पियानो बजाती थीं। वह हमसे कहती, “मुझे मत देखो, अपनी आँखें बंद करो और संगीत सुनो।” इस तरह से मेरे दिमाग में स्वतः ही छवियां सूझने लगीं। यह एक प्रक्रिया है जिसका मैं अब भी पालन करता हूं। मैं इन छवियों में कोई हेरफेर नहीं करता। प्रारंभ में, मुझे छवियों को अपने दिमाग में लाने के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ता था, लेकिन अब वर्षों के अभ्यास के साथ, वे सहजता से प्रवाहित होती हैं। मैंने कभी भी दूसरों के बनाए सिनेमा से कोई छवि उधार नहीं ली है।”
महामारी आने से पहले वे अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू करने की तैयारी में थे। वे अपनी या जीवनानंद दास की कविताओं पर आधारित फिल्में बनाना चाहते थे। मगर सिनेमाहॉल बंद होने के बाद फिल्में बनाना और उन्हें रिलीज करने का इरादा उन्होंने छोड़ दिया।
वे कहा करते थे, “एक फिल्म निर्माता रिटायर हो सकता है, लेकिन छवियां उसे नहीं छोड़तीं। वह छवियों को गले लगाकर सो जाता है और छवियों के साथ जागता है। जब मैं फिल्म नहीं बना रहा होता हूं, तो मुझे कुछ नहीं करना पसंद होता है, मैं सिर्फ अपनी स्मृतियों के साथ बातें करता हूँ। हो सकता है कि फिल्म बनाना अब संभव न हो, लेकिन कोई भी जीवित रह सकता है, कविता लिख सकता है, धुन बना सकता है।”
दिनेश श्रीनेत