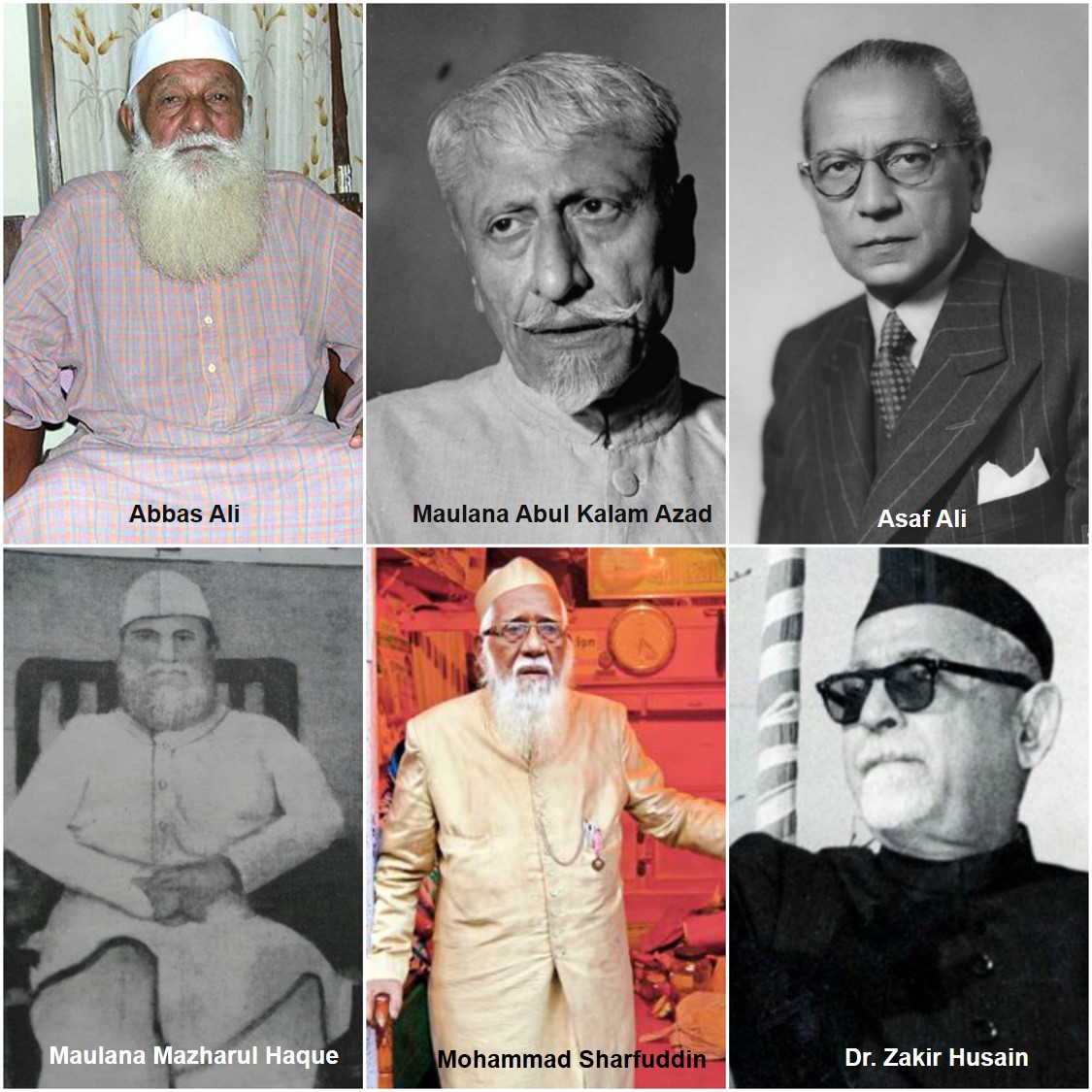इधर दिलीप कुमार की बहुत फ़िल्में देखीं। वही सब, पचास के दशक के आरम्भ की, सफ़ेद-स्याह तस्वीरें। नाटकीय प्रसंगों, भावुक दुविधाओं और सम्बंधों के त्रिकोणों से भरी कहानियां। क्यूं भला, कोई पूछ सकता है। कोई और काम नहीं है क्या? मैं क्या बतलाऊं, काम तो सिर पर हज़ार हैं। न मालूम कितने ही इरादे और मनसूबे- यह करना है, वह करना है, लेकिन दिल कहीं नहीं लगता।
बहुत पहले, लड़कपन में ही यह तमन्ना बांधी थी कि ज़िंदगी में कभी फ़ुरसत मिली तो एक-एक कर दिलीप की फ़िल्में देखूंगा और यह अभिनेता अपनी चुप्पियों से जैसा कोहरा बुनता है, उसके भीतर सिमटकर रहूंगा। वो फ़ुरसत अब मिली है, ये तो न कहूंगा, पर वक़्त के भीतर अब सूने, ख़ाली वक़्फ़े पहले से ज़्यादह हैं। ये वही आलम है, जिसमें दिलीप कुमार के अभिनय से जगने वाली अनुभूतियां गझिन हो जाती हैं।
मैंने हमेशा ही दिलीप कुमार को बहुत पसंद किया, किंतु इधर पहले से पकी उम्र में वो और आत्मीय हो गया है। लड़कपन में सोचता था कि मैंने दिलीप कुमार के जैसे चलना है, उसके जैसे बोलना है। सन् छप्पन-सत्तावन से पहले की फ़िल्मों में उसने जैसे नौजवान का बिम्ब रचा था, मुझे वैसा ही बनना है।
यह चुप्पा, अपने में डूबा हुआ शख़्स- जो मर जाएगा, लेकिन मुंह नहीं खोलेगा। आप कभी जान नहीं सकेंगे कि उसके दिल में क्या था। वह अपना मन किसी को सौंपेगा नहीं, और जब सौंपेगा तो फिर राह से डिगेगा नहीं। किसी ने कहा था, वो सृष्टि का अनादि प्रेमी है। प्यार अगर निष्ठा और आत्मबलिदान का दूसरा नाम है तो उसकी तस्वीर दिलीप कुमार के जैसी बनती है।
अंदाज़ में उसने नरगिस के सामने सिर झुकाकर- जैसे किसी गुनाह का इक़बाल कर रहा हो- मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा था- “मैं आपसे मोहब्बत करता हूं!” उसका वह कहना मेरे ज़ेहन पर नक़्श हो गया। मण्डप सजा था और दुलहन ब्याह के लिए जा रही थी। ऐसे मौक़े पर कौन मोहब्बत का बयान करता है? यह तो अपनी मौत के सामान का बंदोबस्त करने जैसा है। किंतु इसी उलटबांसी का नाम तो दिलीप कुमार है।
जुगनू की तरह चुपचाप जल जाने वाला प्रेमी। विछोह का स्थिरचित्र। उसकी फ़िल्में दु:खान्तों से भरी हैं। प्यार मिल जाए, यह ग़ैरमुमकिन है- इस अहसास का आदमक़द इश्तेहार। उथली सतहों से भरी इस दुनिया में, क्या ही राहत की बात है कि वैसी तलस्पर्शी अनुभूतियों को रचने वाला एक अभिनेता उन्नीस सौ पचास की दहाई में मेरे देश में हुआ था।
मैंने दुनिया की आलातरीन फ़िल्में देखी हैं, उनके सामने फ़िल्मिस्तान और बॉम्बे टॉकीज़ की वो मेलोड्रमैटिक फ़िल्में कुछ भी तो नहीं, जिनमें दिलीप अभिनय करता था। वही तमाम अतिनाटकीय प्रसंग, जिन्हें आने वाले सालों में बम्बइया सिनेमा के द्वारा बूंद-बूंद उलीच लेना था। मनोवैज्ञानिक पर्यवेक्षण से मुक्त ग़ैरब्योरेवार कहानियां, फ़िल्म के परदे पर जिनके निर्वाह में सिने-तकनीक का उत्कर्ष भी नहीं। वो तो पचपन के बाद के सिनेमा में ही दीखना आरम्भ होता है। किंतु मैं तो दिलीप को देखता हूं, उन फ़िल्मों से मुझको सरोकार नहीं। उनसे दिलीप को निकाल दो तो वो निष्प्रभ हैं, कंकाल हैं।
पर दिलीप से मेरी नज़रें हटती नहीं। उसमें चुम्बकीय आकर्षण था। मैं हैरत से देखता कि पूरी फ़िल्म में वो एक बार बेसुरा नहीं होता। एक ग़लत अदा उसके ज़रिये से वाक़य नहीं होती। एक सम्भले हुए क़द के साथ दृश्य में वो मौजूद होता, अपनी बेध देने वाली आंखों और गूंज भरी चुप्पियों के साथ। उधेड़बुन से भरी आत्मा लिए। विष्णु खरे ने दिलीप के लिए कितना वाजिब कहा था- चुप्पी के भीतर एक चुप्पी, अवसाद के भीतर एक अवसाद रचने वाला अभिनेता।
उसकी पहली दो फ़िल्में ज्वार-भाटा और प्रतिमा सफल नहीं रही थीं। रबींद्रनाथ की कहानी नौकाडूबी पर आधारित मिलन से उसने सफलता का स्वाद चखा। सिनेमा की दुनिया में उसके तमाम अभिभावक बंगाली थे और बांग्ला अभिजात्य उसके अभिनय में आरम्भ से ही सज गया। शहीद, शबनम, नदिया के पार में कामिनी कौशल के साथ उसकी जोड़ी ख़ूब जमी, तब वो स्वयं अपनी नायिका जैसा कमनीय नौजवां था। फिर नरगिस के साथ उसकी एक-एक कर परिनिष्ठित फ़िल्में आईं- मेला, अंदाज़, बाबुल, जोगन, दीदार।
हर फ़िल्म के साथ उसका क़द बढ़ता गया। दीदार में उसने आत्मध्वंस के तत्व को पूर्णता से पा लिया। जब वो एक आदिम वहशत के साथ “बुझा दे इन चराग़ों को” कहते हुए अपनी आंखें फोड़ लेता है तो आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। नरगिस उस ज़माने में राज कपूर के प्रेम में डूबी थीं। दिलीप के साथ आई फ़िल्मों में ऐसा मालूम होता रहा कि वो हमेशा उससे एक फ़ासले से मिलती थीं। इसने नाकाम प्रेमी के दिलीप के रूपक को और गहराया ही था।
तराना में मधुबाला के साथ उसको देखकर ऐसा मालूम हुआ, जैसे इस दीवाने को उसका मीत मिल गया है। उस लड़की में एक अनगढ़ खिलंदड़पना था।
उसने दिलीप को सम्हाल लिया। उसे प्रेमल बना दिया। तराना में मधुबाला कहती है- मुझे लगता है तू मुझसे बहुत छोटा है, मेरे बिना तू जाने कहां गिर पड़े, खो जाए। दिलीप आंख उठाकर उसे देखता है और उसकी बात पर यक़ीन कर लेता है। तब लगता है, जैसे वह प्रेमिका में मां की तलाश कर रहा था।
फिर दाग़ का गहरा अवसाद। अमर का अपरिमित अपराध-बोध। शिकस्त की दम घोंट देने वाली बेबसी। वेदना और ग्लानि उसके भीतर गहराती चली गई। उसे आगे चलकर देवदास बनना ही था, देवदास में उसका अभिनय अपनी पूर्णता को ही पा गया।
तब भी, मधुमती उसके अभिनय का उत्कर्ष है। मधुमती में ही उसको और शायद पूरे हिंदोस्तां को ये अहसास भी हुआ कि वैजयन्ती के रूप में उसको अपने जोड़ की साथी मिली है। उसमें नरगिस जैसी निस्संगता नहीं थी, मधुबाला जैसा आवेग भी नहीं। वह ठीक-ठीक दिलीप के द्वारा रचे जाने वाले मिथक के अनुरूप एक नायिका थी। मांग के साथ तुम्हारा, मैंने मांग लिया संसार- दिलीप ने उसके लिए ठीक ही गाया था।
बाद इसके, दिलीप का अभिनय अधिक बहिर्मुखी होता गया। उसने नया दौर, मुग़ले-आज़म, गंगा-जमुना और राम और श्याम में ना केवल अपने कैरियर की सबसे बड़ी हिट फ़िल्में दीं, बल्कि अपने अभिनय के आरम्भिक दौर के संकोच को पूरी तरह तोड़ भी दिया। दिलीप का अभिनेता इन फ़िल्मों में बहुत बुलंद है, किंतु मैं तो दिलीप के पुराने रूपक पर फ़िदा हूं।
वो मुझे मधुमती से पहले की उन फ़िल्मों में ही मिलता है, जब तलत उसके गाने गाता था। कभी-कभी मुकेश। सादे, सुथरे कपड़ों में वह खेत, बाग़, पुलों, पगडंडियों पर टहलता रहता और दु:ख के गाने गाता। दु:ख उसका गहना था। दिलीप को देखकर मुझको लगा कि दु:ख आपको कितना सुंदर बना देता है। इस ज़ेवर को किसी सस्ती चीज़ से बदलने की कोशिश हमने कभी नहीं करना चाहिए।
दिलीप की बहुतेरी फ़िल्में अभी देखना हैं- वो भी जो बहुत क़ामियाब नहीं हुईं- आरज़ू, हलचल, फ़ुटपाथ, इंसानियत। और वो भी, जिनके सिर पर बहुत सहरे सजे- आन, आज़ाद, यहूदी, पैग़ाम। एक-एक कर सभी देख लूंगा। न भी देख पाया तो मुझको हर्ज़ नहीं है। मैंने बहुत सारा पहले ही पा लिया है। अभिनेता एक से एक हिंदी सिनेमा में हुए हैं।
किसी की किसी से तुलना करना जायज़ नहीं। कोई किसी से कमोबेश भी नहीं है। पर जिसके दिल को जो रुच गया, वो उसी का हो रहा- वाला अफ़साना है। मेरे मन को दिलीप कुमार ही सबसे ज़्यादा भाया है। मैं उसके द्वारा प्रस्तुत चरित्रों जैसा ही हमेशा से बनना चाहता था। एक ज़ाती राब्ता दिलीप से है।
आन में जिस नौलखा बाग़ से वह अपनी टमटम दौड़ाकर ले गया था, वह इंदौर शहर की बात थी और मैं उसी नौलखे में फिर छह दहाई बाद रहने को गया था। तब मैं उसके बूढ़े दरख़्तों से बातें करता था और पूछता था- बहुत अरसा हुआ, महान त्रासद-नायक इस डगर से गुज़रा था, क्या तुमको याद है?
बोलो ना, क्या यह सच्चा अफ़साना है? मुझे उन पेड़ों से आज तलक रश्क़ होता है। कि मैं आदमी क्यूं हुआ, सन् इक्यावन में नौलखे बाग़ का दरख़्त क्यूं न हुआ, जिसने दिलीप कुमार को देखा था।
सुशोभित