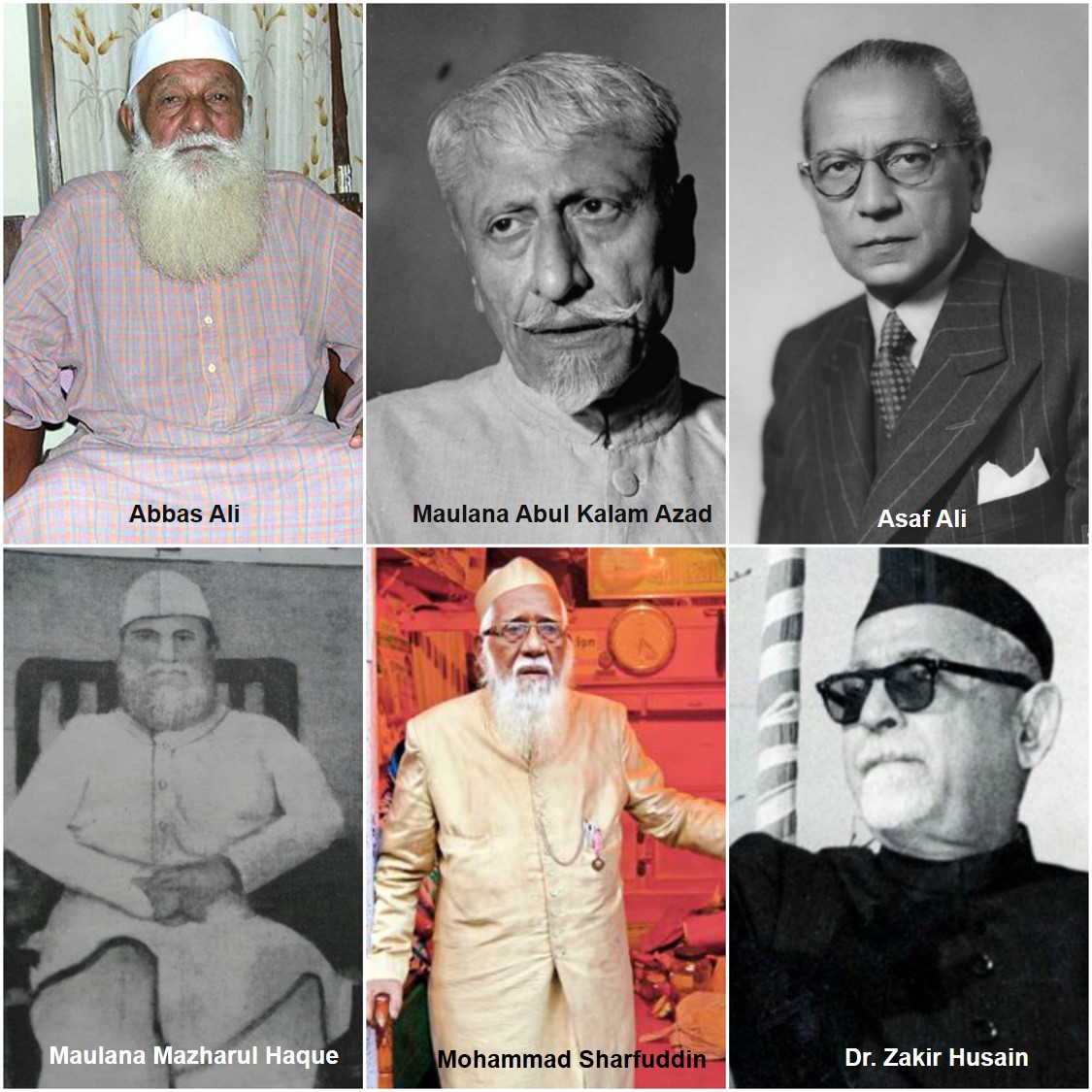8 दिसम्बर ’20 के दिन आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में भारत बंद आयोजित था। दोपहर होते तक भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को बातचीत का निमंत्रण भेज दिया।
लेकिन यह निमंत्रण किसी हल की तलाश की अपेक्षा ‘संदेश’ देने की नीयत से भेजा गया था यह दो बातों से स्पष्ट हुआ। एक तो पूरे किसान प्रतिनिधिमंडल को न बुलाकर चुने हुए लोगों को निमंत्रण दिया गया। संदेश था : फूट डालने के प्रयास का विकल्प हमारे पास है।
लेकिन दूसरा संदेश, बहुत गूढ़ और महत्वपूर्ण, मीटिंग स्थल के चयन के साथ नत्थी हो कर आया।
शुरुआत में बताया गया था बैठक शाम सात बजे गृह मंत्री के निवास में होगी। अंत समय में पता चला स्थान परिवर्तन हो गया है, किन्तु नया स्थान कौन सा है इसको लेकर स्पष्टता नही थी। कुछ किसान समूह विज्ञान भवन गये जहां इससे पहले तक म॓त्रियों के साथ बैठकें हो रही थीं। कुछ नाॅर्थ ब्लाॅक स्थित गृह मंत्रालय की ओर गये तो कुछ एक और संभावित स्थल हैदराबाद हाउस की ओर।
अंततः बैठक विलम्ब से प्रारम्भ हो सकी जब सारे लोगो को अमित शाह की पसंद की ‘वेन्यू’ में पहुंचाया गया।
इस वेन्यू का इतिहास और जड़ कार्पोरेट (ईस्ट इंडिया कम्पनी) के हाथों भारत के किसानों के हुए शोषण और तबाही की याद दिलाता है। हमारे लिये यह इतिहास जानना ज़रूरी है। भारतीय किसान का शोषण करने की दिशा में शासन और कार्पोरेट के बीच के गठजोड़ और दोनों के बीच की जुगलबंदी का इससे बड़ा उदाहरण नहीं है।
ये भी पढ़ें : मोदी कैबिनेट विस्तार: मिशन-2022 की बिसात पर जातीय समीकरण का दांव, क्षेत्रीय संतुलन का भी रखा गया पूरा ख्याल
मीटिंग जहां की गयी उस स्थल का लम्बा औपचारिक नाम था (है) : इंडियन काऊंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। लेकिन आम आदमी इसे ‘पूसा इंस्टीट्यूट’ या बस ‘पूसा’ के प्रचलित नाम से जानता है। भारत में कृषि से जुड़ा आमतौर पर हर व्यक्ति पूसा से परिचित है।
मजे की बात यह है कि पूसा नाम का न तो यहां कोई गांव था न यह किसी व्यक्ति का नाम था। पूसा शब्द दरअसल एक बड़े नाम का संक्षिप्त रूप है। जैसे न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथाॅरिटी के अंग्रेज़ी के पहले अक्षरों को मिला कर बना शब्द “नाॅएडा”; या नाॅर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऐजेन्सी इलाके के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द “नेफा”। (1972 में इसका नाम अरुणाचल राज्य रखा गया और नेफा इतिहास का भाग बना)
पूसा की अंग्रेजी स्पेलिंग के चार अक्षरों को पूरा लिखा जाये तो बनेगा – ” फिप्स (ऑफ) यूनाइटेड स्टेट (ऑफ) अमेरिका।
आइये जानें कौन थे फिप्स और क्या थी कहानी जो पूसा को भारतीय कृषि इतिहास का अभिन्न हिस्सा बना गयी।
ईस्ट इंडिया कम्पनी ने किसानों को ज़मीन का मालिकाना हक़ अवश्य दिया पर टैक्स में बेइन्तिहा बढ़ोतरी कर दी। अधिक आमदनी के लालच (या दबाव) ने किसानों को नील, अफीम, कपास, चाय और काॅफी जैसी नगद फसल उगाने के लिये मजबूर किया। उत्पादन वृद्धि में मदद के नाम पर नहरों का जाल बिछाया गया। पर टैक्स में वृद्धि और अधिक हो गयी। खेतों में उत्पादन कम हुआ और बाद में खेत की मिट्टी अनाज उत्पादन के लायक नहीं बची। उधर अनाज उत्पादन के लिये पर्याप्त खेत भी नहीं बचे थे।
अकाल पड़ना शुरू हो गये, भुखमरी के कारण बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण मरने लगे। किन्तु कम्पनी (और 1860 के बाद ब्रिटिश सरकार) का सारा ध्यान उत्पादन बढ़ाने की ओर था।
बिहार के दरभंगा ज़िले में एक बहुत बड़ा इलाका कम्पनी के कब्ज़े में था। शुरू में कई वर्षों तक इस स्थान का उपयोग कम्पनी की फौज के लिये उन्नत नस्ल के घोड़ों के स्टड फार्म के रूप में किया गया। स्टड फार्म चला और बंद हो गया। खाली पड़ी ज़मीन को 1878 में इंग्लैंड की एक कम्पनी ने तम्बाखू उत्पादन के लिये लीज़ पर लिया तब पहली बार इस एस्टेट का साईज़ रिकाॅर्ड में दर्ज हुआ – 1350 एकड़। तम्बाखू कारोबार जम नहीं पाया तो कम्पनी ने 1897 में यह स्थान खाली कर दिया।
दो वर्षों के बाद वर्ष वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्ज़न ने कार्यभार संभाला।
कर्ज़न ने भारतीय पुरातत्व के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किये। लावारिस पड़े ताजमहल को सरकारी संरक्षण देना उनमें शामिल है। सांची, सारनाथ, तक्षशिला आदि में उत्खनन जैसे और भी काम किये।
लेकिन इतिहास बहुत क्रूर होता है। शासक लाख अच्छे काम करे इतिहास उसे उसी काम के लिए याद रखता है जिसके विरोध में जनता सड़क पर उतर आती है।
अपने शासन के छह साल पूरे होने पर आत्मविश्वास से भरे कर्ज़न ने बंगाल का विभाजन कर पूर्वी बंगाल और असम के नये प्रांत बना दिये। जनता विरोध में सड़कों पर उतर आयी। सरकार संशोधन का विकल्प सुझाती रही। जनता नहीं मानी। विरोध जारी रहा। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और कानून वापस हुआ।
लेकिन वापस चलते हैं और कर्ज़न के काल की उस घटना की ओर जिसका संबंध इस कहानी से है।
कर्ज़न का काल वह दौर था जब अंग्रेज़ प्रशासकों पर भारत की कृषि व्यवस्था को लेकर दो तरफा दबाव था। लंदन से दबाव था कि कृषि व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व में बढ़ोतरी की जाए। साथ ही योरोप में हो रहे औद्योगिक विकास के कारण कपास जैसे ‘राॅ-मटीरियल’ की सप्लाय बढ़ाने का दबाव था। दूसरी तरफ योरोप के उन व्यवसायियों (आज की भाषा में कार्पोरेट घरानों) का दबाव था जो ब्रिटिश सरकार के दिखाये सपनों पर विश्वास कर भारत के कृषि क्षेत्र में अपना निवेश बहुत बढ़ा चुके थे किन्तु अब उम्मीद के अनुपात में कम होते लाभ को ले कर आक्रोशित थे।
कृषि क्षेत्र में उत्पादन और अधिक चाहिए था, लाभ और अधिक चाहिए था। और कर्ज़न के सामने यह लक्ष्य हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती थी।
लॉर्ड कर्ज़न का विवाह जर्मन मूल की अमरीकी महिला मेरी विक्टोरिया लीटर के साथ हुआ था। मेरी विक्टोरिया, जो विवाह के बाद बैरोनेस कर्ज़न के रूप में जानी गयीं, के पिता की गिनती अमेरिका के सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में होती थी। इनके घनिष्ठ मित्र थे शिकागो के रहने वाले हेनरी फिप्स। ये दोनों अपने तीसरे मित्र ऐन्ड्रयू कार्नेगी के स्टील उद्योग में बड़े निवेशक थे ।
अमरीकी पूंजीवादी व्यवस्था में प्रचलित कानून के अनुसार यदि उद्योगपति अपने मुनाफे की राशि को घर में या बैंक में रखने की बजाए ऐसे उद्यमों या प्रयोजनों के लिये दान करता है जो आगे चलकर उद्योग को और अधिक मुनाफा दिलाने का माद्दा रखते हो तो ऐसे दान पर उसे टैक्स आदि में भारी छूट दी जाती है। इस नीति ने अमेरिका में राॅकफैलर से लेकर बिल गेट्स तक अनेक दानदाता पैदा किये हैं।
हेनरी फिप्स के मित्र की बेटी का विवाह भारत के सबसे शक्तिशाली अधिकारी के साथ हुआ तो फिप्स भी अपने लिये संभावनाओं की तलाश में भारत पहुंचे और लाॅर्ड कर्ज़न के मेहमान के रूप में रुके। यहां की व्यावसायिक संभावनाओं ने फिप्स को आकर्षित किया और उन्होने तीस हज़ार डाॅलर का दान दिया। घोषणा हुई कि इसका उपयोग ब्रिटिश भारत में फसलों का उत्पादन और कृषि क्षेत्र से मुनाफा बढ़ाने के तरीके ढूंढ़ने (रिसर्च) के लिये किया जाएगा। जो इसे विकास की ओर कदम न मानें उनके शब्दों में ‘निचोड़ ली गयी किसानी से और अधिक रस प्राप्त करने के तरीके ढूँढे जाएंगे’।
स्थान के रूप में चयन किया गया वही दरभंगा का 1350 एकड़ का एस्टेट जो टोबैको कम्पनी के जाने के बाद से वीरान पड़ा था। इस स्थान पर 1 अप्रेल 1905 के दिन लाॅर्ड कर्ज़न ने कृषि रिसर्च के लिये एक संस्थान के भवन का शिलान्यास किया। भवन के डिज़ाइन को लेकर कर्ज़न मुतमईन नहीं थे। वे चाहते से विशेषज्ञों से सलाह मशविरा कर लिया जाए। किन्तु जल्द-से-जल्द लाभ-प्राप्ति के लिये आतुर बैठे ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव में सब काम रिकाॅर्ड गति से हुआ। दान की राशि का मूल्य 45 लाख रुपयों के बराबर था। शिलान्यास भी हुआ और देखते देखते इमारत के साथ कैम्पस भी खड़ा हो गया।
अब तक चले आ रहे बेनाम एस्टेट का पहली बार नामकरण हुआ: फिप्स (Phipps) ऑफ यू.एस.ए. के नाम पर – पूसा। संस्था का नाम हुआ इम्पीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट।
15 जनवरी 1934 के दिन भूकंप आया और समूची विशाल इमारत भरभरा कर ध्वस्त हो गयी। अब तलाश शुरु हुई नये स्थान की। तीन साल पहले ही भारत की राजधानी के रूप में नयी दिल्ली का उद्घाटन हुआ था।
भारत की बड़ी समाचार ऐजेन्सी ए. एन. आई. के संस्थापक प्रेम प्रकाश जी की लिखी पुस्तक ‘रिपोर्टिंग इंडिया’ इसी माह प्रकाशित हुई है। सन् चालीस के दशक की दिल्ली का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं कि करोल बाग के आस-पास का इलाका वीरान था, रहने योग्य नहीं था। अपेक्षाकृत छोटे वृक्षों वाले घने जंगल थे जिन्हे आज भी ‘रिज’ के नाम से जाना जाता है।
1935 में इसी रिज का विशाल इलाका चुना गया और दरभंगा के मलबे से उठाकर पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली पहुंचा दिया गया। आठ दिसम्बर 2020 को कृषि क्षेत्र में काॅरपोरेट घरानों की घुसपैठ कराने में सरकार की भूमिका पर संदेह करते हुए जब किसानों ने ‘भारत बंद’ का आह्वान किया तो दिल्ली में उपलब्ध सारे विकल्पों को छोड़कर गृह मंत्री ने उनसे बातचीत के लिये यही स्थान चुना।
अमित शाह का निर्णय महज़ संयोग था या प्रयोग यह बाकी लोगों के लिए अनुमान का विषय है।
डाॅ. परिवेश मिश्रा