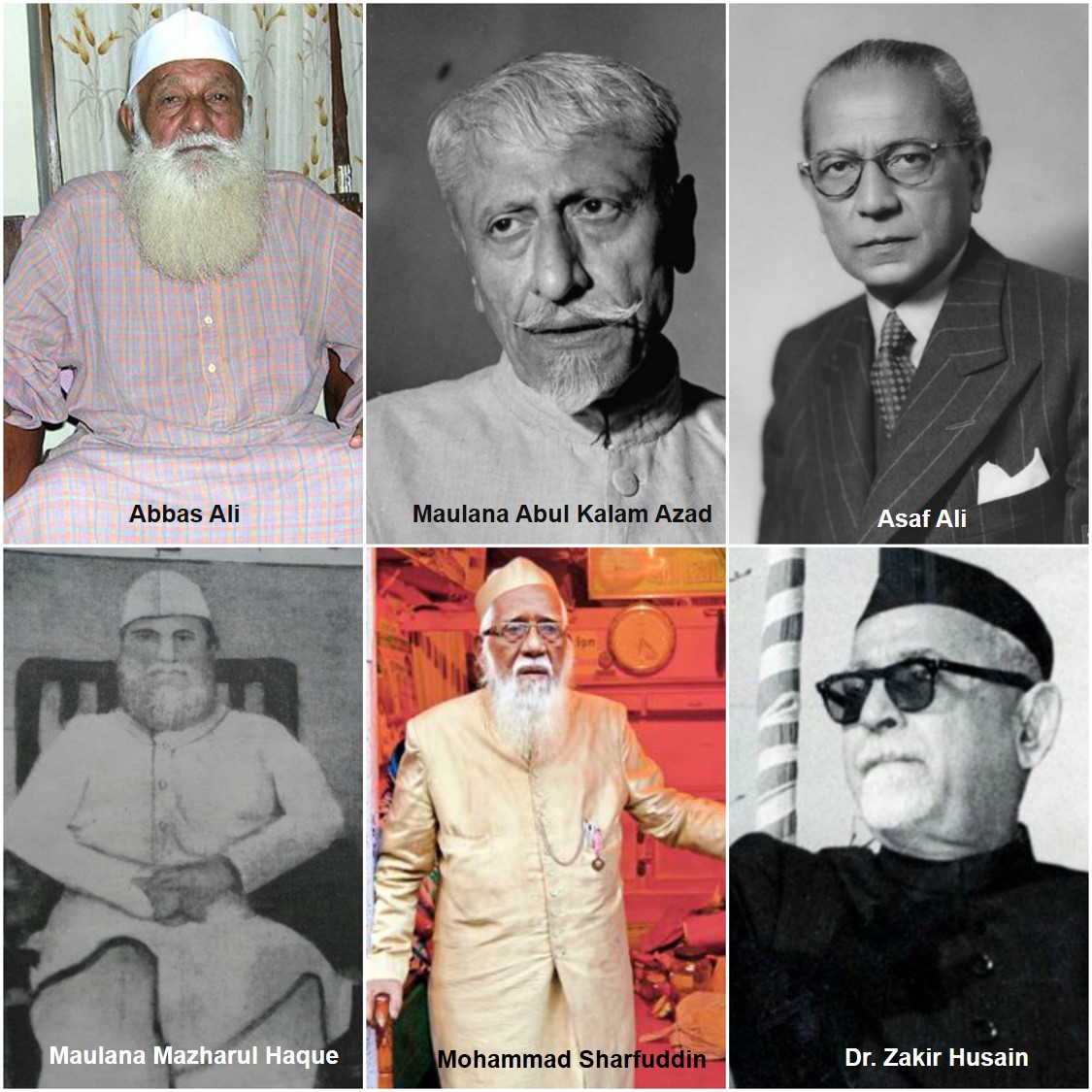गुरुवार को उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाएंगे। चुनावी पंडित पूर्वानुमानों का खेल खेलने में व्यस्त हैं। यह अलग बात है कि जनता ऐसे पूर्वानुमानों को हमेशा से धता बताती रही है। 1984 के चुनावों में कई अख़बार राजीव गांधी की हार की घोषणा कर रहे थे। मगर जनता ने राजीव गांधी को 400 से ज़्यादा सीटें दे डालीं।
कुछ अख़बारों ने माफ़ी मांगी। 2004 में अटल-आडवाणी की अपराजेय लगती जोड़ी हार को राजनीति में नौसिखिया नज़र आने वाली सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए ने मात दी थी। 2014 में किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा अपने बूते बहुमत ले आएगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ऐसी बंपर जीत की उम्मीद या घोषणा किसी ने नहीं की थी।
तो सारे पूर्वानुमान राजनीति और पत्रकारिता का खेल हैं। जनता का फ़ैसला इनसे अलग है। लेकिन क्या जो फैसला आएगा वह वाकई जनता का ऐसा निर्दोष फैसला होगा जिसकी अपेक्षा हमारा संसदीय लोकतंत्र करता है? जाने-अनजाने हमने संसदीय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति को एक-दूसरे का पर्याय बना डाला है। निस्संदेह चुनाव लोकतंत्र की प्राथमिक शर्त हैं लेकिन वे इकलौती शर्त नहीं हैं। एक मज़बूत लोकतंत्र सिर्फ़ चुनाव से नहीं बचता, उसे और भी संस्थाएं बचाती हैं। चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और प्रशासन स्वतंत्र होते हैं तो लोकतंत्र स्वस्थ होता है।
दुर्भाग्य से हमारे यहां चुनावी राजनीति जितना परवान चढ़ी है, दूसरी लोकतांत्रिक संस्थाएं उतनी ही कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। चुनावी राजनीति धीरे-धीरे या तो पूंजी के खेल में बदलती जा रही है या फिर जाति और संप्रदाय के ऐसे समीकरण में, जिनमें बुनियादी मुद्दे खोए हुए हैं। जनता राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों पर नहीं, नेताओं के निजी जादू पर वोट कर रही है। ऐसा व्यक्तिवाद अंततः लोकतंत्र के लिए नुक़सानदेह होता है। दरअसल यह लोकतांत्रिक तरीक़े से ही लोकतंत्र का खात्मा करने जैसा है। ऐसा नहीं कि यह सिर्फ़ भारत में हो रहा है।
स्टीवन लेवित्स्की और डेनियल ज़िब्लैट ने अपनी किताब ‘हाउ डेमोक्रेसीज़ डाई’ में इस बात का परीक्षण किया है कि कैसे अमेरिका के चौकस लोकतंत्र के भीतर डोनाल्ड ट्रंप जैसा तानाशाह प्रवृत्ति का नेता सेंधमारी करने में सफल रहा। वे लिखते हैं कि अब लोकतंत्र को फौजी बूटों और संगीनों से नहीं, बिल्कुल लोकतांत्रिक तौर-तरीकों से नष्ट किया जाता है।
तुर्की की लेखिका ऐस तेमलकुरेन ने अपनी किताब ‘हाउ टू लूज़ अ कंट्री: सेवेन स्टेप्स फ्रॉम डेमोक्रेसी टू डिक्टेटरशिप’ में बताया है कि किस तरह राष्ट्रवादी और मज़हबी उन्माद को बढ़ावा देते हुए वहां बरसों से लोकतंत्र के चुपचाप अपहरण और रूपांतरण का खेल जारी है।
वे लिखती हैं कि तुर्की में हम समझते थे कि जो हुआ, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगली बार उससे भी बुरा हो जाता। फिर हम मानते कि अब इससे ज़्यादा पतन तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर नई गिरावट हमारा मुंह चिढ़ाती।
क्या इसमें कोई शक है कि हमारा लोकतंत्र भी ऐसे ही ख़तरों से घिरा हुआ है? हमारी संसद और विधानसभाओं में दाग़दार और पैसे वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या बड़ी होती जा रही है। वे जैसे यह साबित करने पर तुले हैं कि जनता द्वारा चुन लिए जाने भर से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। पार्टियां जनता की राय भी ख़ारिज कर देती हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा के जिन तीन सौ से ज़्यादा विधायकों को सदन में भेजा, उनमें से किसी को पार्टी ने मुख्यमंत्री नही बनाया।
बहरहाल, 2022 को 2024 का सेमीफ़ाइनल कहा जा रहा है। हालांकि इतिहास ऐसे भी सेमीफ़ाइनलों की तस्दीक नहीं करता। 2003 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीतने के बाद 2004 में भाजपा चुनाव हार गई थी और 2007 में मायावती के हाथों यूपी को गंवा देने के बावजूद 2009 में कांग्रेस ने अपनी सीटें बढ़ा ली थीं।
फिलहाल, बहुत सारे सवालों से घिरे लोकतंत्र में तत्काल जो सबसे प्रासंगिक सी बात लग रही है वह डॉ राम मनोहर लोहिया ने बरसों पहले कही थी। उनका कहना था कि सत्ता की रोटी को पलटते रहना चाहिए, नहीं तो वह जल जाती है। क्या जनता अपनी रोटी का स्वाद बचाना चाहती है? गुरुवार को इस सवाल का जवाब मिलेगा।