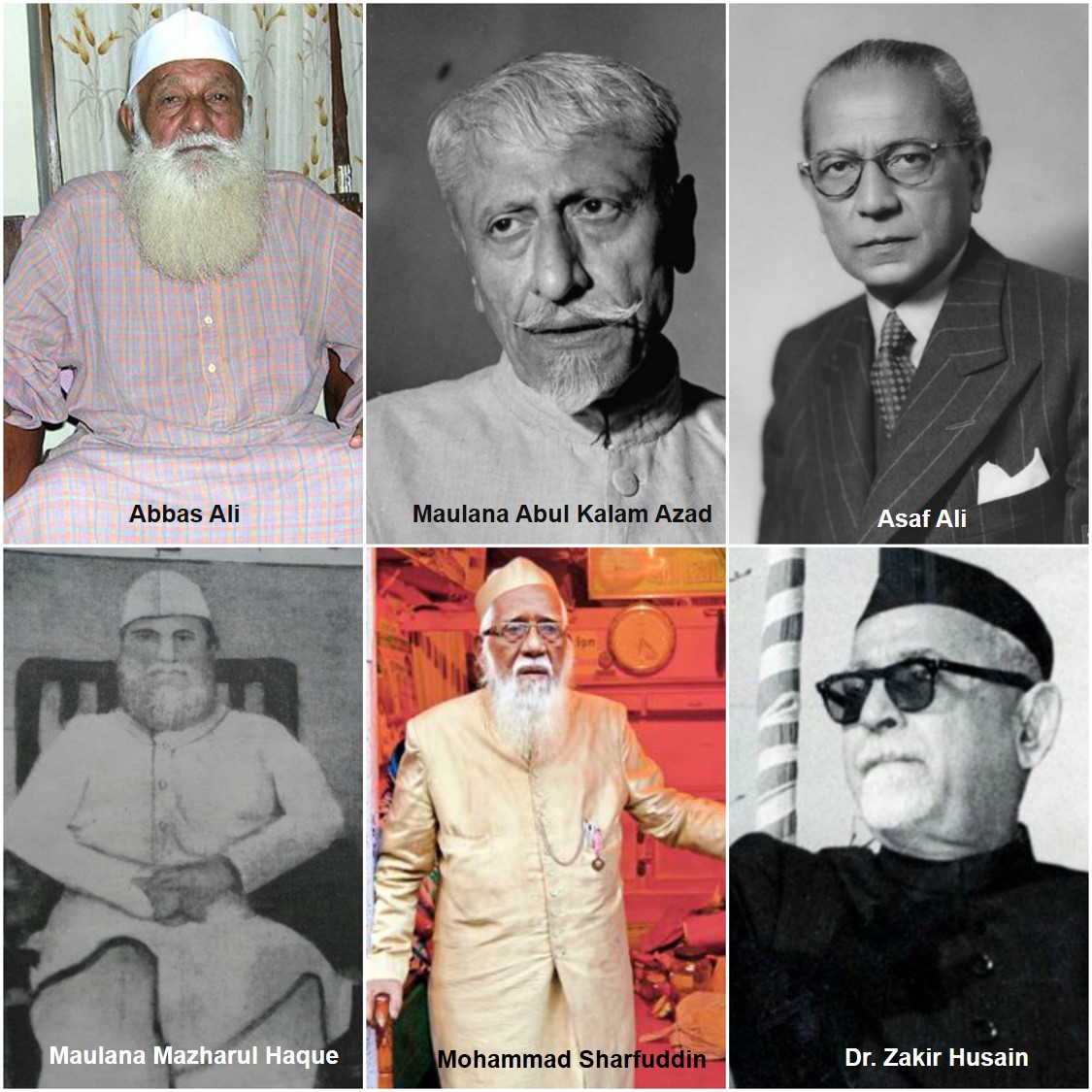उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर राज्यों में विधान सभा चुनावों के लिए प्रचार से पोस्टर पटे पड़े हैं। लेकिन कहीं भी इस प्रचार में मज़दूर आंदोलन नहीं है। ट्रेड यूनियंस अब मुख्य धारा की राजनीति से बाहर हैं। कहीं भी ‘बोल मज़ूरा हल्ला बोल!’ जैसे आंदोलित और एकजुट कर देने वाले नारे अब नहीं गूंजते।
तो क्या माना जाए, कि मज़दूर आंदोलन अब समाप्त हो चुका है? अथवा मज़दूरों की एकजुटता अब नहीं रही? जबकि इन सभी राज्यों में औद्योगिक विकास हुआ है। फ़ैक्ट्री और कारख़ाने नए लगे हैं। सरकारी और स्वायत्तशासी निकायों में कर्मचारी भी बहुत हैं। किंतु नहीं बचा तो कर्मचरियों का कोई आंदोलन। मोटे तौर पर इसका जवाब है, सोवियत संघ के विघटन के बाद से दुनिया जिस तरह उदारवाद और खुली अर्थ व्यवस्था की तरफ़ दौड़ी, उसमें मज़दूर आंदोलन ख़त्म होते गए।
लेकिन इसमें एक शंका भी है, दुनिया के विकसित देशों में मज़दूर आंदोलन भले न हों पर वहाँ सेवायोजकों को मज़दूरों को सभी बुनियादी सुविधाएँ देनी पड़ती हैं। ट्रेड यूनियंस के दबाव में वहाँ सेवायोजक मज़दूरों के लिए निर्धारित सुविधाएँ देने से मना नहीं कर सकते। भले वहाँ दक्षिणपंथी सरकारें हों या समाजवादी रुझान वाली सोशल डेमोक्रेट। किंतु सोशल सिक्योरिटी को लेकर वहाँ जन-दबाव इतना अधिक रहता है, कि कोई भी सरकार इससे मुँह नहीं चुरा सकती।
इसके विपरीत भारत में मज़दूर आंदोलन को लेकर कोई जन दबाव नहीं है। बंगाल जहां 34 वर्षों तक माकपा की सरकार रही, वहाँ यह प्रचारित किया गया कि कोलकाता से उद्योगों के पलायन के पीछे कम्युनिस्ट सरकारें और ट्रेड यूनियन मूवमेंट रहे।
लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं दे सका, कि जब वहाँ माकपा के मुख्यमंत्री बुद्धदेब भट्टाचार्य ने सिंगूर में टाटा को नैनो कार की फ़ैक्ट्री डालने के लिए हज़ार एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण को मंज़ूरी दी थी, तब क्या हुआ था? इसी तरह कैसे नंदी ग्राम को विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर किया गया? इन सब बातों से एक बात तो पता चलती ही है कि पूरे देश में बड़े कल-कारख़ानों के विरुद्ध कुछ लोगों ने मुहीम चलाई। उद्योगपतियों को लाभ इसमें था, कि किसी तरह एक कारपोरेट कल्चर विकसित की जाए और मज़दूरों को फुटकर क्षेत्र में डाला जाए।
अर्थात् वर्क फ़ोर्स की आउट सोर्सिंग। इससे उस कम्पनी का मालिक मज़दूरों से कोई वास्ता नहीं रखता। वह यह भी कोशिश करता है, कि उसकी कम्पनी में प्रोडक्ट की सिर्फ़ असेंबलिंग हो। इसमें गुणवत्ता तो देखी जाएगी लेकिन मज़दूरों का बोझ मालिक पर नहीं पड़ेगा। बड़ी सफ़ाई से मज़दूर मुख्यधारा से ग़ायब हो गए। और जब मज़दूर ही संगठित नहीं हो पा रहे तो उनका कैसा आंदोलन!
यही कारण है कि सारे औद्योगिक शहरों में माल तो बन रहा है, लेकिन मज़दूर नहीं दिखते। जो स्किल्ड लेबर है वह ख़ुद छोटा-बड़ा कांट्रेक्टर है। इसके अतिरिक्त मशीनीकरण, कम्प्यूटर क्रांति ने मज़दूरों पर निर्भरता कम कर दी। ऑटोमेशन का यह युग यद्यपि 1980 से शुरू हुआ था, लेकिन 2000 आते-आते सारे बड़े कारख़ाने बंद हो गए। मालिकों के लिए यह आह्लाद का वक़्त था, क्योंकि उनकी मिलें शहरी प्राइम इलाक़े में आ गई थीं।
उनकी ज़मीनों की जो क़ीमत आंकी गई वह मुनाफ़े पर चलने वाले कारख़ाने से कहीं अधिक थी। संगठित मज़दूर तो बेकार हो गया, वह दिहाड़ी की मज़दूरी करने लगा, जिसमें न भविष्य था न कोई हितलाभ। किसी भी सरकार ने इन मज़दूरों की तरफ़ ध्यान नहीं दिया। कितनी विचित्र बात है, कि किसी भी औद्योगिक शहर में आज मज़दूरों की सुधि लेने वाला कोई आंदोलन नहीं है। और राजनीतिकों को भी यही रास आता है कि वे पब्लिक का सांप्रदायिक अथवा जातीय ध्रुवीकरण कर दें। यह अकेला विकल्प है, जिस पर चल कर बड़े मज़े से वोट पाए जा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक शहर कानपुर में तो 1980 के पहले तक हर चुनाव में मज़दूर ही तय करते थे, कि शहर का लोकसभा में विधान सभा में कौन प्रतिनिधित्व करेगा। 1952 से 1989 तक संसद और विधायिका में मज़दूरों का कोई न कोई प्रतिनिधि रहा अवश्य। यह मज़दूर राजनीति का ही कमाल था जो बैंक, रेलवे, ऑर्डिनेंस फ़ैक्ट्रीज़ में भी कामगारों की यूनियनें बहुत ताकतवर हुआ करती थीं।
1980 के दशक तक कानपुर में एक कोने से दूसरे कोने तक “बोल मज़ूरा हल्ला बोल!” का नारा गूंजता था। उस समय कानपुर में 65 ऐसी मिलें, कारख़ाने थे, जहां हज़ार से ऊपर मज़दूर कार्यरत थे। तब यह शहर मिलों के भोंपू से जागता था और इन्हीं भोंपुओं की कर्कश ध्वनि से सोता था। लेकिन तब यह शहर जीवंत था।
हर मिल के समक्ष हज़ारों और लोगों को रोज़गार मिलता था। पान वाले, चाय वाले, पकौड़ियाँ तथा चाट बेचने वाले, साबुन, तेल, बनियायन और जाँघिया बेचने वाले, साइकिल का पंचर जोड़ने वाले। शहर में तीन लाख से ऊपर तो मिल मज़दूर थे और लाख के ऊपर वे लोग, जिनको ये मज़दूर रोज़गार देते थे। एक तरह से कानपुर मज़दूरों की ज़िंदादिली से जीवंत था।
बहुत से लोग मानते हैं, कि दुनिया में मज़दूर आंदोलन अर्थात् कम्युनिस्टों का आंदोलन! जबकि ऐसा नहीं है। मज़दूर आंदोलन मनुष्य जाति के मिथकों में भी मौजूद हैं। कई बार अत्याचारी शासकों के दमन से प्रजा को बचाने के लिए आंदोलन हुए। बस माइथोलॉजी आंदोलन के नेता का नाम ही याद रखती है, इसलिए आंदोलन के कारणों को हम भूल चुके हैं।
मिस्र की एक लोक कथा के अनुसार इस से 1800 वर्ष पहले ‘हयक्ष’ नाम की एक खानाबदोश जाति ने भैरव साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। यही नहीं प्रगति प्रकाशन मास्को से प्रकाशित पुस्तक- “संक्षिप्त विश्व इतिहास” में पहला जन आंदोलन दासों के विद्रोह को माना है। स्पार्टकस के नेतृत्त्व में शुरू हुआ यह विद्रोह ईसा पूर्व 74 वर्ष से ईसा पूर्व 71 वर्ष तक चला। भारत में भी इस तरह के विद्रोह के कई उदाहरण हैं।
आंध्रभ्रत्य में लिपिकों का आंदोलन चला। लेकिन संगठित मज़दूर आंदोलन 19वीं सदी में चले। हाँ यह ज़रूर है कि सबसे पहले 1847 में कम्युनिस्ट लीग ने ही ‘दुनिया के मज़दूरो एक हो’ का नारा दिया था। 1871 में पेरिस कम्यून बना, जो मज़दूर राज्य था। एक मई 1886 को शिकागो में काम के घंटे कम करवाने को ले कर औद्योगिक मज़दूरों ने प्रदर्शन किया। कई मज़दूर पुलिस की गोली से मारे गए। किंतु जीत मज़दूरों की हुई और काम के घंटे तय किए गए।
भारत में पहला मज़दूर आंदोलन 1877 में हुआ था। नागपुर की एक सूती मिल के मज़दूरों ने हड़ताल की। चूँकि कानपुर में भी सूती मिलों की क़तार में पहली मिल- एलगिन मिल 1861 में स्थापित हुई थी, इसलिए यहाँ भी मज़दूर काम के लिए आने लगे। ये वे मज़दूर थे जो गाँवों में भारी और नक़द के रूप में ही लगान देने की बाध्यता के चलते अपनी कृषि ज़मीनें खो चुके थे। इनको और कुछ नहीं आता था। न कोई कौशल इनके पास था न व्यापार करने की कला इनको पता थी।
इसलिए अपना श्रम बेचने के अतिरिक्त इनके पास और कोई विकल्प नहीं था। ऐसे लोग कानपुर आने लगे। 1876 में कानपुर वूलेन मिल्स (लाल इमली) की स्थापना हुई और इसके बाद तो यहाँ कारख़ानों की झड़ी लग गई। गाँव से मज़दूर आते और मिलों में काम करने लगते। तब भारत में मज़दूरों के न तो काम के घंटे तय थे न वेतन समान होता था। छुट्टी भी नहीं मिलती थी। मिल मालिक, जो कि अधिकतर अंग्रेज थे, मज़दूरों से मारपीट भी करते। एक तरह से मज़दूरों के साथ ग़ुलामों जैसा व्यवहार होता था।
सबसे पहले कांग्रेस नेता बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में मज़दूरों को एकजुट कर उनकी स्थितियों को सुधारने का आंदोलन चलाया। लाहौर में लाला लाजपत राय सक्रिय हुए। कलकत्ता में जूट मिल मज़दूरों की यूनियन बनी। कानपुर में पंडित पंडित कामदत्त और लाला देवी दयाल ने मज़दूरों को एकजुट करने का प्रयास किया। ये दोनों एलगिन मिल के हवाघर में काम करते थे।
कानपुर में तिलक के कट्टर अनुयायी थे मौलाना हसरत मोहानी और गणेश शंकर विद्यार्थी। इन्हीं की प्रेरणा से पंडित कामदत्त ने ग्वाल टोली में 19 नवम्बर 1919 में कानपुर मज़दूर सभा की स्थापना की। ‘कानपुर: मज़दूर आंदोलन का इतिहास’ नामक पुस्तक में लेखक सुदर्शन चक्र ने लिखा है, कि कई मज़दूर इस सभा में रहे और इन्हें नामी कांग्रेस नेता मुरारी लाल रोहतगी, गणेश शंकर विद्यार्थी तथा मौलाना हसरत मोहानी का सहयोग था।
शहीद भगत सिंह, राधा मोहन गोकुल जी जैसे तमाम लोग कानपुर आ कर मज़दूरों के बीच काम करने लगे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कानपुर में हुआ और कानपुर में मज़दूर आंदोलन इतना तेज हो गया कि आज़ादी के समय से ही लगने लगा था कि कानपुर में चुनाव वही जीत सकता है, जिसे मज़दूरों का समर्थन हो।
यही कारण रहा कि 1952 के पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने मज़दूर नेता हरिहर नाथ शास्त्री को लोकसभा के लिए टिकट दिया और कानपुर ईस्ट से विधान सभा के लिए टिकट सूर्य प्रसाद अवस्थी को। अवस्थी भी मज़दूर नेता थे।
हरिहर नाथ शास्त्री मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले और जाति से कायस्थ थे। लेकिन उस समय जाति और जातियों का गठजोड़ कोई मायने नहीं रखती थी। उनकी जीत की वज़ह उन पर मज़दूरों का भरोसा और कांग्रेस की टिकट थी। उस समय कानपुर के मज़दूर जवाहर लाल नेहरू को अपना लेनिन मानते थे। कामरेड सुदर्शन चक्र के आल्हा में नेहरू जी के लिए यही संबोधन है-
“हिंद के लेनिन को अब सुमिरौं, जिसका नाम जवाहर लाल।
शोषक वर्ग नाम से काँपे, समझें जिसे आपना काल।।”
मज़दूरों के लिए यही पर्याप्त था।
इसीलिए 1952 में हरिहर नाथ शास्त्री जीते। लेकिन 1953 की दिसम्बर में नागपुर जाते समय एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उपचुनाव में शिव नारायण टंडन जीते। हालाँकि वे बड़े व्यापारी थे किंतु उनके संबंध भी मज़दूरों से थे। 1954 में उन्होंने नेहरू जी की नीतियों से मतभेद के चलते लोकसभा से इस्तीफ़ा दे दिया। फिर उपचुनाव हुआ और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर मज़दूर नेता राजाराम शास्त्री जीते।
यह भी दिलचस्प है, कि 1952 में कानपुर दक्षिण-इटावा लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर ही बाल कृष्ण शर्मा ‘नवीन’ जीते। नवीन जी मूल रूप से मध्य प्रदेश के शाजापुर के थे। दसवाँ पास करने के बाद उनकी मुलाक़ात माखन लाल चतुर्वेदी से हुई। वे उन्हें कानपुर ले कर आ गए। माखन लाल जी ने उनकी भेंट गणेश शंकर विद्यार्थी से करवाई। उनके आग्रह पर नवीन जी ने क्राइस्ट चर्च कॉलेज से बीए किया और विद्यार्थी जी के अख़बार ‘प्रताप; में संपादक हुए साथ ही कांग्रेस से जुड़े और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से भी।
तब तक यह संस्था कांग्रेस के पास ही थी बाद में यह कम्युनिस्टों के पास चली गई। नवीन जी हिंदी के बहुत अच्छे कवि थे और उनकी ओजस्वी कविताएँ कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को प्रेरित करती थीं। नेहरू जी उन्हें पसंद करते थे। वे उन्हें संविधान सभा में भी लाए और 1952 में कानपुर दक्षिण से लोकसभा में भी। 1957 में वे राज्यसभा में आए।
हरिहर नाथ और राजाराम दोनों ही काशी विद्यापीठ से पढ़े थे और दोनों पर लाला लाजपत राय का असर था। लेकिन 1957 से कानपुर लोकसभा सीट की फ़िज़ां बदल गई। हालाँकि सीट मज़दूर नेता के पास रही, लेकिन कम्युनिस्टों के पास चली गई। मज़दूर नेता एसएम बनर्जी ने यह सीट 1957 से 1977 तक पूरे 20 साल अपने पास रखी। 1957, 1962 और 1967 का लोकसभा चुनाव वे निर्दलीय किंतु सीपीआई के सपोर्ट से जीते। 1971 में कांग्रेस और सीपीआई में पैक्ट था इसलिए उनको कांग्रेस (इंदिरा) का भी समर्थन रहा। जबकि पहले के तीनों चुनावों में कांग्रेस ने उनके विरोध में प्रत्याशी उतारे।
1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोहर लाल ने उन्हें हरा दिया। 1980 में कांग्रेस के आरिफ़ मोहम्मद ख़ान और 1984 में नरेश चंद्र चतुर्वेदी जीते। आरिफ़ का कानपुर से कोई ताल्लुक़ नहीं था किंतु नरेश जी नीचे से ऊपर पहुँचे थे और मज़दूर राजनीति में भी उनका दख़ल रहा। 1989 में वीपी सिंह ने जो जन मोर्चा बनाया था था, उसे सीपीएम का सपोर्ट था।
समझौते में यह सीट सीपीएम को मिली और यहाँ से मज़दूर नेता सुभाषिणी सहगल जीतीं। सुभाषिणी स्वयं मज़दूरों के बीच सक्रिय रही थीं जबकि उनकी माँ डाक्टर लक्ष्मी सहगल नेता जी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फ़ौज (आईएनए) की सेनानी राह चुकी थीं। उन्होंने ही रानी झांसी रेजीमेंट बनाई थी। वे पेशे से चिकित्सक लेकिन अद्भुत वीरांगना थीं।
कानपुर की विधानसभा सीटों पर भी मज़दूर नेता ही जीतते रहे। भले वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से रहे हों या कांग्रेस के अथवा सीपीआई के। सरयू प्रसाद अवस्थी के बाद उमेश चंद्र शुक्ल, प्रभाकर त्रिपाठी, गणेश दत्त वाजपेयी, मौलाना संत सिंह यूसुफ़ और गणेश दीक्षित भी विधायक रहे। ये सभी मज़दूर राजनीति से आए थे। कानपुर में सीपीएम की ट्रेड यूनियन सीटू का कोई प्रत्याशी कभी नहीं चुनाव जीता। जबकि सीटू के लोग सर्वाधिक जुझारू रहे हैं। कामरेड रामासरे, कामरेड दौलत राम कभी चुनाव नहीं जीत सके।
जबकि कानपुर का मज़दूर आंदोलन का इतिहास कामरेड रामासरे के बिना अधूरा रहेगा। रामासरे के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओत्सेतुंग से रिश्ते थे। कलकत्ता में एक बार जब मुख्यमंत्री बुद्ध देब भट्टाचार्य से मेरी मुलाक़ात हुई और मैंने कहा, सर आई एम फ़्रॉम कानपुर तो वे तपाक से बोले- ओह द सिटी ऑफ़ कामरेड रामासरे। एक तरह से रामासरे कानपुर की पहचान थे। लेकिन वे चुनाव नहीं जीत सके।
पूरे उत्तर प्रदेश में कानपुर ही ऐसा शहर था, जहां मज़दूर आंदोलन ने संगठित रूप लिया था। कम्युनिस्ट पार्टियाँ तो उत्तर प्रदेश में ग़ाज़ीपुर, वाराणसी, बांदा और अयोध्या, फ़ैज़ाबाद तथा हरदोई से भी कई बार जीती हैं किंतु मज़दूरों के नेताओं ने कानपुर में ही अपना सॉलिड वोट बैंक तैयार किया था।
लेकिन 1980 आते-आते मज़दूर आंदोलन भी बिखरा और मज़दूर नेता भी अपनी साख खोते गए। अब न जड़ों वाले कम्युनिस्ट नेता बचे हैं न वे समर्पित मज़दूर आंदोलन। कानपुर के मज़दूर आंदोलन की कब्र पर अंतिम कील तब ठुकी जब 6 दिसंबर 1977 को स्वदेशी गोलीकांड हुआ और 11 मज़दूर मारे गए थे।
क़रीब ढाई सौ लोग घायल हुए थे। दरअसल वेतन न मिलने से अकुलाए मज़दूरों का धैर्य चुक गया और उन्होंने प्रबंधन का घेराव किया। कोई नेता उन्हें सँभाल नहीं सका और एकाउंटेंट शर्मा तथा प्रोडक्शन मैनेजर आयंगर को मज़दूरों ने बॉयलर में फेक दिया था। इसके बाद मज़दूर आंदोलन बिखर गया।
शंभूनाथ शुक्ल