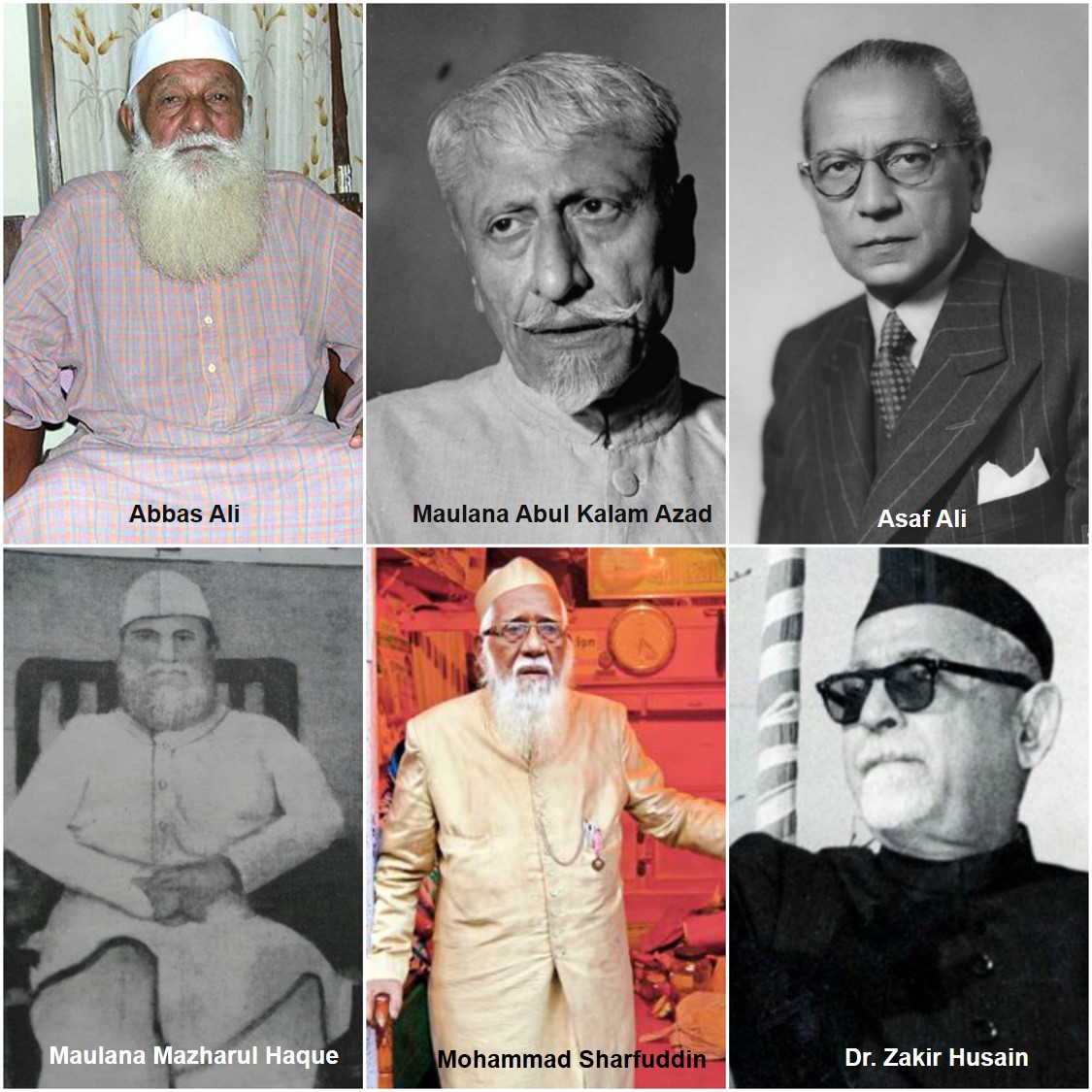धरती के अलावा किसी और अंतरिक्षीय पिंड पर पांव रखने का मौका इंसान को पहली बार ईसवी सन 1969 में मिला था। उस साल की 21 जुलाई को यह कार्य संपन्न करने वाले सज्जन थे कोरिया में युद्ध लड़ चुके अमेरिकी नेवी के टेस्ट पायलट और ऐरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर नील आर्मस्ट्रांग। इसे मानव सभ्यता के एक नए युग का प्रारंभ बताया गया। अगले तीन साल तक कई अपोलो यान अंतरिक्षयात्रियों समेत चांद पर गए। लेकिन जैसे ही अमेरिका को लगा कि यह बहुत ही खतरनाक और खर्चीला सौदा है और बदले में चांद से उसे कुछ मिलने वाला भी नहीं है, वैसे ही न सिर्फ उसने चंद्रयात्राओं का सिलसिला खत्म कर दिया, बल्कि तब से अबतक नजारा कुछ ऐसा बना हुआ है, जैसे यह पूरी बात ही सिरे से झूठी रही हो।
और तो और, इंसान को चांद तक ले जा सकने वाली रॉकेट टेक्नॉलजी भी नए सिरे से खड़ी करनी पड़ रही है, जैसे पुरानी कहीं खो गई हो। आखिरी अपोलो यान, अपोलो-17 सन 1972 में चांद पर गया था और अब, उसके आधी सदी बाद आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत जो मानव रहित अंतरिक्ष यान चांद से थोड़ा आगे तक ले जाकर वापस धरती पर ले आने की योजना बनाई गई है, उसे करीब नौ महीनों में यह काम मुख्यतः सौर ऊर्जा के बल पर पूरा करना है। जाहिर है, अपोलो मिशन से इसकी सीधे कोई तुलना नहीं की जा सकती।
इंसान को चांद तक ले जाने और फिर वहां से वापस लाने वाले यान को इस काम में हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। तीन लोगों की टीम के लिए जरूरत भर की हवा-पानी, रसद और कामकाज से लेकर वापसी तक का ईंधन ढोने की क्षमता जिस सैटर्न रॉकेट में थी, वह इंसान का बनाया हुआ अभी तक का सबसे ताकतवर, सबसे खर्चीला और सबसे ज्यादा प्रदूषण पैदा करने वाला रॉकेट था। एलन मस्क का दावा सैटर्न से सस्ता, कम हानिकर और उसके समतुल्य शक्ति वाला रॉकेट बना लेने का है। लेकिन यह रॉकेट एक हफ्ते से ज्यादा लंबा मानवयुक्त मून-मिशन संपन्न कर ले जाएगा, ऐसा तो कोई दावा भी उन्होंने नहीं किया है।
चीनी खेमा, अमेरिकी खेमा
अभी सिर्फ इतना तय है कि अमेरिका इस साल से चांद पर स्थायी रूप से डेरा गिराने की मुहिम शुरू कर रहा है। और पचास साल पहले निपट चुके अपोलो अभियान के बरक्स इस बार की मुहिम में वह अकेले नहीं जा रहा। दुनिया की तीन और बड़ी स्पेस एजेंसियां, जिनका संबंध यूरोप, जापान और कनाडा से है, इस मुहिम में उसके साथ हैं। इन तीन के अलावा मेक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, इटली, यूक्रेन, पोलैंड और लग्जेमबर्ग की स्पेस एजेंसियों के साथ नासा ने आर्टेमिस समझौते पर दस्तखत किए हैं। समझौता यह कि इस मुहिम के तहत किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रयोगों और चंद्र-संसाधनों के दोहन में उनकी किसी न किसी तरह की साझेदारी हो सकती है।
इससे जुड़ने का न्यौता रूसियों के पास भी गया था लेकिन उनका कहना है कि पूरे अभियान का बहुत ज्यादा अमेरिका-केंद्रित रूप देखकर उनकी अंतरिक्ष संस्था रोसकोसमोस ने इससे हाथ खींच लिए। इसके बजाय चीन के साथ मिलकर एक समानांतर चंद्र-अभियान का हिस्सा बनना उसे बेहतर विकल्प लगा, लेकिन इस फैसले का एक सैन्य पहलू भी है, जिसपर अलग से बात होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि चंद्रमा से जुड़े प्रयोगों में हमारा पड़ोसी मुल्क चीन फिलहाल अमेरिका समेत बाकी दुनिया से बहुत आगे है। इस वायुशून्य पिंड पर मौजूदा सदी में सफलता पूर्वक अपना रोवर उतारने, लंबे समय तक जमीनी प्रेक्षण लेते रहने और चंद्रमा से 1 किलो 731 ग्राम नमूने लेकर लौटने का श्रेय सिर्फ उसे ही जाता है।
इन नमूनों में ऊपरी धूल और पत्थरों के अलावा अलग-अलग गहराइयों से (अधिकतम एक मीटर नीचे से) लिए गए सैंपल भी शामिल हैं, जिन्हें देश भर में फैली खनिज प्रयोगशालाओं को खोजबीन के लिए बांट दिया गया है। चीन के दो रोवर झूरोंग और यूटू-2 आज भी चीन पर मौजूद हैं और उनके प्रेक्षण दुनिया भर में चर्चा का विषय बने रहते हैं। इनमें ज्यादा खास है यूटू-2, जो पिछले तीन वर्षों से चांद पर अपनी मौजूदगी के दौरान कुल 900 मीटर की दूरी ही तय कर पाया है। इसकी वास्तविक उपलब्धि अत्यंत विषम परिस्थितियों में इतने लंबे समय तक काम करते रहने की है।
कैसा है चांद पर होना
चंद्रमा की परिस्थितियां कितनी विषम हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए कुछ तथ्यों पर गौर करें। यूटू-2 चंद्रमा की दूर वाली सतह पर है, जिसका सामना पृथ्वी से कभी नहीं होता। कंट्रोल रूप से उसका संपर्क एक चीनी चंद्र-उपग्रह के जरिये सीमित अवधि के लिए ही हो पाता है। चंद्रमा का एक दिन धरती के 29 दिनों के बराबर होता है। यूं कहें कि वहां के रात और दिन अलग-अलग धरती के साढ़े चौदह-साढ़े चौदह दिनों के बराबर होते हैं। घंटे भर में 600 मीटर चल सकने वाला यूटू-2 वहां सूर्योदय के समय एक बार में सिर्फ दो-तीन मीटर चलता है और 360 डिग्री कैमरे के जरिये ली गई अपने परिवेश की तस्वीरें चीन स्थित कंट्रोल रूम में भेज देता है।
उसके कंट्रोलर आस-पास मौजूद छोटे-छोटे कंकड़ों तक का हिसाब रखते हैं, फिर उनसे बचते हुए यूटू-2 का आगे का रास्ता तैयार करते हैं। इस बात को जरा और बेहतर ढंग से समझें। यूटू-2 के पास हमेशा चलते रहने की सुविधा नहीं है। चंद्रमा की लंबी और अत्यंत ठंडी रातें उसको किसी पत्थर के टुकड़े की तरह बितानी होती हैं। साढ़े चौदह दिन तक पारा माइनस 173 डिग्री सेल्सियस- कभी थोड़ा कम, कभी थोड़ा ज्यादा दिखाता है! फिर जब इतना ही लंबा दिन उगता है तो दोपहर होते-होते तापमान प्लस 127 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है।
जाहिर है, धरती के अधिकतम ठंडे और गर्म इलाकों में इन दोनों चरम तापमानों का आधे से एक तिहाई हिस्सा ही उपलब्ध हो पाता है। इनमें काम करना तो दूर, बचे रह सकने वाले सोलर सेल और बाकी चीजें भी अलग लेवल की विशेषज्ञता मांगती हैं। अपोलो मिशन के दौरान चंद्रयात्रियों का टाइम टेबल तय था कि उन्हें चंद्रमा पर सूर्योदय के समय ही यान से बाहर आना है और सूर्यास्त से पहले रॉकेट दागकर अंतरिक्ष में लौट आना है। यूटू-2 अगर तीन साल से चांद पर सक्रिय है तो इसका अर्थ यह हुआ कि चीनी स-शरीर नहीं तो कम से कम रोबॉट के जरिये वहां काम कर सकते हैं।
रूसियों ने 1973-74 में चांद पर लूनोखोद नाम की अपनी गाड़ी 26 मील दौड़ाई लेकिन उनका मकसद वहां सिर्फ फोटो लेने और कुछ चट्टानों की स्पेक्ट्रोग्राफी करने तक सीमित था। इसे गर्म रखने के लिए उन्होंने रेडियो ऐक्टिव पदार्थ पोलोनियम-210 का इस्तेमाल किया था, हालांकि इससे जुड़ा उनका पहला प्रयोग धरती पर ही विफल हो गया था और इस खतरनाक चीज के अवशेष रूस में जगह-जगह फैल गए थे। आने वाले चंद्र अभियानों में चीन के साथ रूसियों के रिश्तों का आधार क्या बनेगा, कहना कठिन है क्योंकि उनके लिए यह बहुत पहले छोड़ दिया गया रास्ता नए सिरे से पकड़ने जैसा ही होगा।
लेकिन धातु विज्ञान (मेटलर्जी) में रूसियों को दुनिया में सबसे आगे समझा जाता है और अमेरिकी स्पेस शटल का किस्सा खत्म होने के बाद से इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली रॉकेट साइंस के तो वे चैंपियन ही हैं। ऐसे में उम्मीद है कि 2035 में चांद पर ठिकाना बनाने का अपना लक्ष्य यह खेमा भी हासिल करके रहेगा। ध्यान रहे, हमारे इसरो के लिए इन दोनों ही खेमों के दरवाजे खुले हुए हैं। इनमें से किसी एक में शामिल होना है या चांद को लेकर अपने अलग रास्ते पर ही डटे रहना है, यह फैसला किसी दिन हमें भी करना होगा।
दो रणनीतियों का फर्क
दोनों अभियानों के प्रस्ताव पढ़ने से ऐसा लगता है कि अमेरिका का जोर अपना अड्डा चंद्रमा की सतह के बजाय उसकी कक्षा में कायम करने पर है, जबकि चीनी अपना बेस कैंप सतह पर ही बनाना चाहते हैं और चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे स्पेस स्टेशन को समर्थक भूमिका में रखना चाहते हैं। अमेरिकियों ने अपने अड्डे को ‘गेटवे’ नाम दे रखा है, जो एक चर्चित साइंस फिक्शन का शीर्षक भी है। हालांकि ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि चंद्रमा की तरफ अमेरिका की वापसी चीनियों के इस दिशा में काफी आगे बढ़ जाने के कारण ही हो रही है।
चंद्रमा पर पाया जाने वाला कम से कम एक खनिज हीलियम-3 पहली नजर में उसे आर्थिक दृष्टि से आकर्षक बना रहा है। लेकिन अव्वल तो जिस फ्यूजन एनर्जी के लिए एक आदर्श ईंधन की भूमिका यह निभा सकता है, वह अभी दूर की चीज है- कम से कम 2040 के बाद की। दूसरे, इस खनिज का कुल हिस्सा चंद्रमा के दूर वाले इलाके की धूल में एक अरब कणों के पीछे 50 कण का ही है। इसे निकालने का कोई आसान तरीका अगर खोज लिया गया तो भी सस्ता ईंधन यह हरगिज नहीं होगा।
अभी इस काम के लिए हाइड्रोजन के दो आइसोटोपों ड्यूटीरियम और ट्रिटियम का इस्तेमाल करने की बात है, जिनमें दूसरा वाला दुर्लभ है और समुद्री जल से उसे निकालना बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन इसे फ्यूजन रिएक्टर में लीथियम टाइल्स पर हाई स्पीड न्यूट्रॉनों के प्रहार के जरिये बना लेने का एक प्रस्ताव भी है, जो अगर कामयाब हो गया तो चंद्रमा से हीलियम-3 लाने वाली बात उतनी आकर्षक नहीं रह जाएगी।
चंद्रमा की सतह पर खोजी अड्डा बनाने को लेकर दो विचार हैं। एक तो यह कि लावा ट्यूब्स के रूप में कोई प्राकृतिक गुफा अपने हाथ लग जाए। इसे लेकर कई बारीक सर्वे किए जा चुके हैं और 200 संभावित जगहों में से कुछेक पर फोकस भी किया जा रहा है। लेकिन असल आइडिया थ्री-डी पेंटिंग के जरिये वहीं के मटीरियल से तैयार किए गए कंक्रीट से छोटे-छोटे इगलू नुमा घर बनाने का है। चंद्रमा की धूल को पिघलाकर उसमें पिघला हुआ गंधक मिलाने से ऐसा कंक्रीट तैयार हो सकता है, ऐसी एक उम्मीद वैज्ञानिकों को है, जिसे जमीन पर उतारने का काम इस दशक में शुरू हो जाएगा।
निश्चित रूप से चांद पर इंसानों की दूसरी पारी वहां से माल-असबाब बांधकर लाने की उम्मीद से नहीं शुरू की जानी चाहिए। मानवजाति के लिए सूचना और ज्ञान बाकी किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी हैं। फिलहाल इन्हें ही वहां से अर्जित करने और बेहतर तरीके से धरती पर लाने के उपाय सोचे जाएं, तो भी कोई हर्ज नहीं है।