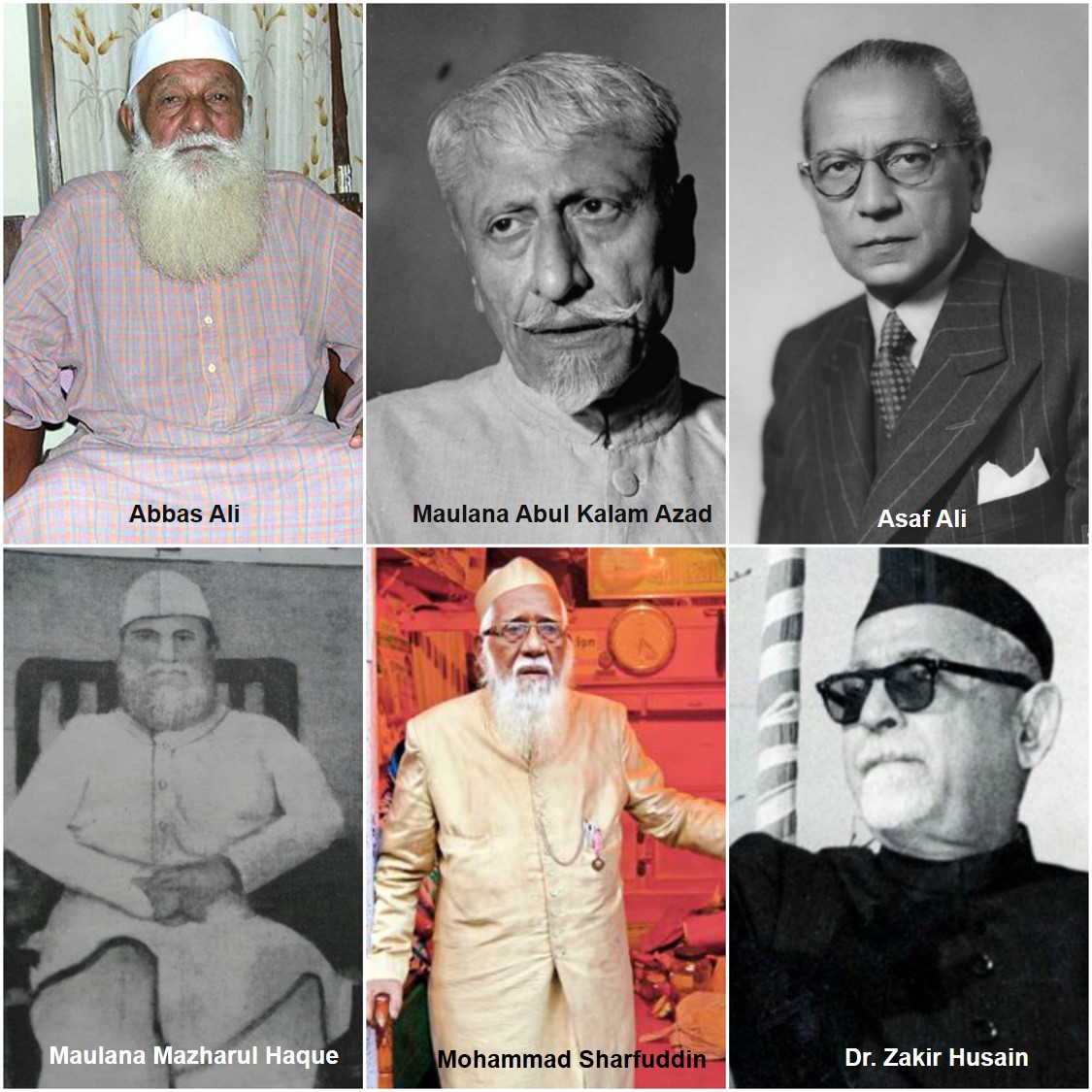कुंदनलाल सहगल का घराना परफेक्शन का घराना था. दुःख उस सधी हुई आवाज का स्थाई भाव था जिसमें करोड़ों हिन्दुस्तानियों को अपनी आत्मा का सबसे चमकीला प्रतिविम्ब नजर आया. यह अकारण नहीं है कि खोजने पर आज भी देश के हर नगर-कस्बे में धुंधुआती निगाह और खरज-भरी आवाज वाला अस्सी-नब्बे साल का एक न एक ऐसा बूढ़ा मिल जाएगा जो कुंदनलाल सहगल को हूबहू गाता हो – “गम दिए मुस्तकिल, कितना नाज़ुक है दिल.”
कुंदनलाल सहगल की आवाज हमारे पास सत्तर-अस्सी साल पहले के दौर तक जाने का सबसे मजबूत और पायेदार पुल है. हिन्दी फ़िल्मी गीतों की सुदीर्घ, समृद्ध परम्परा इसी आवाज से शुरू होती है. 14-15 बरस के करियर में कुल फ़क़त 185 गानों के साथ सहगल ने जो लकीर खींची हिन्दी फिल्मों का कोई भी गायक उसे पार न कर सका – मोहम्मद रफ़ी भी नहीं.
ये भी पढ़ें : जैक लंदन की लिखी एक कहानी
उनके हिन्दी गानों की कुल संख्या 110 है. बाकी भाषाओं में गाई रचनाओं को छोड़ दें तो उन्होंने मिर्जा ग़ालिब, शेख इब्राहीम जौक और सीमाब अकबराबादी जैसे उस्तादों को भी गाया. मिर्जा ग़ालिब को सबसे अच्छा गाने वालों में उनका नाम ख़ासा ऊपर रहेगा. निखालिस सोने में ढले उनके सुरों ने जीवन के राग पर अपनी पकड़ कभी ढीली नहीं होने दी.
उनका जीवनवृत्त घर से भागे किसी लड़के की फन्तासी सरीखा है. जम्मू रियासत के तहसीलदार अमरचन्द सहगल के घर 1904 में 11 अप्रैल के दिन कुल पांच में से चौथी औलाद के रूप में जन्मे कुंदनलाल को बचपन से ही मां के साथ मंदिरों में जाकर भजन सुनने-गाने का शौक लग गया. मां केसरदेवी को गाने का शौक तो था लेकिन पति के कठोर अनुशासन के सामने उनकी वह प्रतिभा जीवन भर दबी रही. अमरचन्द गाने-बजाने को भांड-मीरासियों का काम मानते थे. लेकिन बालक कुंदन ने अभिनय का शौक भी पाल लिया. सुरीली आवाज के चलते स्थानीय रामलीला में उन्हें सीता का रोल करने को मिलता था.
जम्मू में सूफी संत सलामत यूसुफ का मशहूर डेरा था जहाँ होने वाली नशिस्तों में जाना शुरू करने के बाद कुंदनलाल सहगल को क्लासिकल गायकी के अंगों – ख़ास तौर पर ठुमरी और ग़ज़ल से लगावट पैदा हुई. पिता की लगातार झिड़कियों और पढ़ाई में मन लगाने की नसीहतों से आजिज़ आकर उन्होंने पहले दिल्ली जाकर रेलवे में टाइमकीपर की नौकरी की और उसके बाद अस्सी रुपये माहवार पर रेमिंगटन कंपनी के टाइपराइटर बेचे.
जीवन के अगले पड़ावों में पहले कलकत्ता फिर बंम्बई पहुंचने, फिल्मों में गाना-अभिनय करने और बहुत कम समय में देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाने की उनकी तमाम कहानियां पढ़ने-सुनने को मिलती हैं. उनका जीवन इस तथ्य की तस्दीक करता है कि किस तरह एक अकेले आदमी ने अपनी सधी हुई मजबूत आवाज के दम पर करीब डेढ़ दशक तक समूचे देश के संगीत को काबू किया. हिन्दी फिल्मों में ईमानदार आवाज की वैसी साध फिर किसी गले में नहीं आ सकी. उन्हें सुनते हुए अपनी आवाज आज भी रुंध जाती है.
18 जनवरी 1947 को गुजर गए कुंदनलाल सहगल का 43वां जन्मदिन तीन माह बाद आना था.
सहगल भारतीय सिनेमा का पहला कल्ट थे जिन्होंने अकेले दम पर फिल्मी संगीत को एक पुख्ता चरित्र दिया, उसे आकार में ढाला. दुखों और अनुभवों की भट्टी में तपकर उन्होंने खुद को लोहा बनाया. वही लोहा उनकी आवाज की तनी हुई रीढ़ है जिसके सामने नए गवैये टीन के पत्तर जैसे बजते हैं.
उन्होंने एक बार कहा था – “मैं कोई गायक नहीं हूँ. मेरे पास किसी भी तरह की क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं है सिवा उसके जिसे मैंने सुना और याद कर लिया. मुझे एक तरह से समझ में आता है कि मालकौंस में धैवत या मध्यम को किस तरह महसूस होना चाहिए, और यह कि निषाद की प्रकृति कैसी होती है. एक राग के दूसरे में जाने पर ये चीजें बदलती चलती हैं. भैरवी मेरा सबसे प्रिय राग है. भैरवी को जानने का मतलब हुआ सारे रागों को जान लेना.”
उनके पास क्लासिकल की वाकई ज़रा भी औपचारिक ट्रेनिंग नहीं थी. कड़ी मशक्कत और स्वाध्याय से उन्होंने अपना संगीत हासिल किया था.
उनकी मृत्यु के तीस साल बाद राघव मेनन ने अपनी किताब में उन्हें “सुर का तीर्थयात्री” बताया तो मशहूर अंगरेजी कवि आगा शाहिद अली ने अपनी एक कविता में उनके सुरों को “गले में अटकी मौत” कह कर संबोधित किया.
हरमंदिर सिंह ‘हमराज’ और हरीश रघुवंशी की 2004 की किताब ‘जब दिल ही टूट गया’ में कलकत्ते के न्यू थियेटर के संगीतकार आर. सी. यानी राय चन्द्र बोराल के हवाले से एक किस्सा है.
1930 की दहाई के शुरुआती सालों में फिल्म निर्देशक के तौर पर नितिन बोस का बड़ा नाम था. आर. सी. बोराल ने उनसे कुंदनलाल सहगल की सिफारिश की तो उन्हें झिड़कते हुए बोस बोले, “अगर मैं कभी गलती से भी अपना कैमरा इस आदमी पर फोकस करूँ तो उसके लेंस में दरार पड़ जाएगी. वह इस कदर गंवार है!”
बाद में इन्हीं नितिन बोस की तमाम हिट फिल्मों में सहगल ने ही मुख्य भूमिकाएं निभाईं. उनकी असमय मृत्यु नितिन बोस के लिए बहुत गहरा सदमा थी जिससे उबरने के लिए उन्होंने सहगल की याद को कभी धुंधला न होने देने का निश्चय कर लिया और 1955 में दो घंटे की एक फिल्म बनाई जिसका नाम था – ‘अमर सहगल’.
अशोक पांडेय