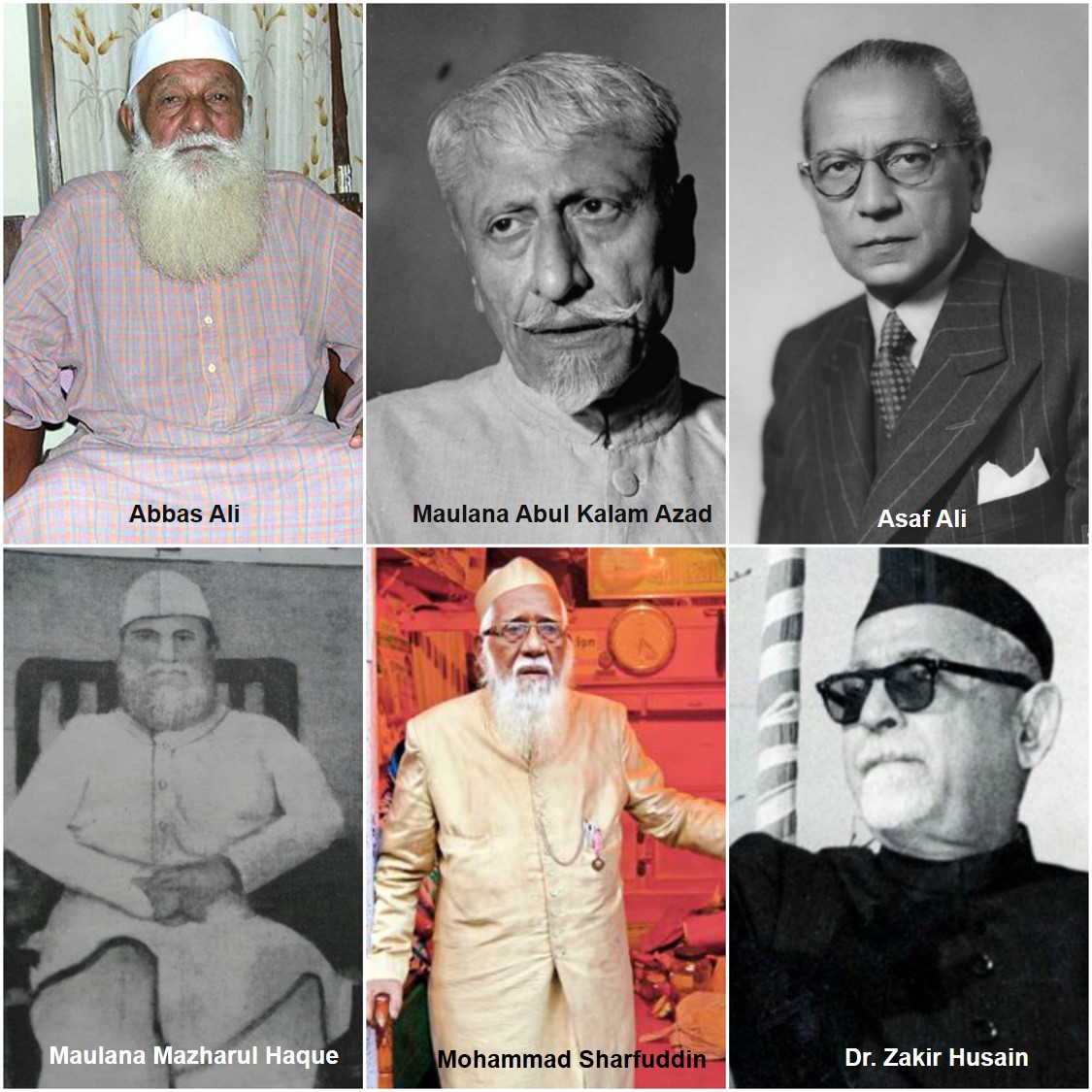काम और बेहतर मौक़ों की तलाश में सिख दुनिया के कोने-कोने में गए हैं. साल 1884 में सिख शंघाई पहुंचे.
शंघाई के रहने वाले छाओ यिन बीज़िंग के शिंघुआ विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय इतिहास और भारत-चीन संबंधों के बारे में पढ़ाते हैं.
पिछले साल उन्होंने शंघाई के सिखों पर एक किताब लिखी – फ़्रॉम पुलिसमैन टू रेवोल्यूशनरीज़, सिख डायस्पोरा इन ग्लोबल शंघाई.
ये किताब उन सिखों की कहानी है जो 1884 में पंजाब से शंघाई पहुंचे, कैसे उन्हें शंघाई पुलिस फ़ोर्स में नौकरी मिली और किन परिस्थितियों में उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शंघाई छोड़ना पड़ा.
छायो यान के मुताबिक एक वक़्त था जब शंघाई में क़रीब ढ़ाई हज़ार सिख रहते थे, लेकिन आज शंघाई में सिख नज़र नहीं आते. ऐसा क्यों है कि इस सवाल का सीधा जवाब उनके पास भी नहीं.
सिंगापुर में सिखों की एक बड़ी जनसंख्या देखकर उन्होंने शंघाई, सिंगापुर और हॉन्ग कॉन्ग सिख समुदाय के बारे में किताब लिखने के बारे में सोचा.
यान के मुताबिक साल 1884 में सबसे पहले सिख शंघाई हॉन्ग कॉन्ग से पहुंचे ना कि पंजाब से. उनकी तादाद 30 के आसपास थी. हॉन्ग कॉन्ग में ये सिख पुलिस विभाग में काम करते थे.
ब्रितानी अधिकारियों ने इन सिखों को शंघाई में नौकरी दी और ये लोग पुलिसकर्मी और वॉचमैन के तौर पर काम करने लगे.
ये सिख पुलिसकर्मी जल्दी ही साल 1854 में बनी शंघाई म्यूनिसिपल पुलिस का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए.

छायो यान कहते हैं, “शंघाई में इन सिखों को पुरानी नौकरियों से कहीं ज़्यादा तन्ख्वाह मिलती थी. इस कारण यहां बड़ी संख्या में सिख आने शुरू हो गए.”
शंघाई के स्थानीय लोगों ने जब सिखों को अपने शहर में पुलिसवालों की वर्दी में देखा तो उनकी प्रतिक्रिया मिली-जुली थी.
छायो यान बताते हैं, “ब्रितानी अधिकारियों को लगा कि स्थानीय लोग सिख पुलिसवालों की अजीब सी पगड़ी और कपड़े, लंबी दाढ़ी से डरते थे. दूसरी तरफ़ चीन के कई लोगों ने सिख पुलिसवालों का स्वागत किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लोग चीनी पुलिसवालों से कम भ्रष्ट थे.”
किताब के मुताबिक चीन के अपराधी चीनी पुलिसकर्मियों से नहीं डरते थे, उन्हें नीची निगाह से देखा जाता था और यहां तक कि उनकी बेइज़्ज़ती भी की जाती थी.
साल 1880 के आसपास शंघाई में ब्रिटेन, फ़्रांस जैसे देश आपस में सहयोग कर रहे थे.
ये दौर पहले अफ़ीम युद्ध के बाद का दौर था जब मुख्य रूप से ब्रितानी, फ़्रेंच और अमरीका के साथ लड़ाई में हार के बाद चीन को विजयी सेनाओं को आर्थिक रियायतें देनी पड़ी थीं.
छायो यान बताते हैं, “जब चीन के लोगों ने फ़्रांस के खिलाफ़ मोर्चा खोल दिया तो ब्रिटेन के अधिकारियों को इससे चिंता हुई. उन्होंने शंघाई की सुरक्षा मज़बूत करना शुरू किया. उन्हें पता चला कि अंग्रेज़ों को शंघाई में पुलिस विभाग में नौकरी देना काफ़ी महंगा था. उन्हें स्थानीय चीनी पुलिसवालों पर भी भरोसा नहीं था, कि कहीं लड़ाई के दौरान वो धोखा न दे दें. तब उन्होंने हॉन्ग कॉन्ग से पुलिस विभाग में सिखों की भर्ती शुरू की, क्योंकि हॉन्ग कॉन्ग शंघाई के नज़दीक था.”
हॉन्ग कॉन्ग के सिख पुलिसवालों को चीनी लोगों के साथ व्यवहार का तजुर्बा भी था.
शुरुआत में करीब 30 सिख शंघाई आए, लेकिन धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी. इसका कारण ये भी था पंजाब और पंजाब के बाहर संदेश गया कि शंघाई में सरकार दूसरी जगहों के मुक़बले बहुत अच्छे पैसे दे रही है, इसलिए कई सिख खुद शंघाई पहुंचने लगे.
किताब के मुताबिक साल 1906 में शंघाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (एसएमसी) ने पहले गुरुद्वारे को अनुमति दी. लोगों को हॉन्ग कॉन्ग भेजा गया ताकि वहां बने गुरुद्वारे से जानकारी हासिल की जा सके और आख़िरकार जून 1908 में उत्तरी सिचुआन में एक गुरुद्वारा बना.
किताब के मुताबिक़, “एसएमसी को उम्मीद थी कि इस गुरुद्वारे से शंघाई के सभी सिखों जैसे पुलिसकर्मियों, वॉचमैन और बेरोज़गारों पर शासन करने में मदद मिलेगी. इस गुरुद्वारे में ग़रीब और बेघर सिखों को जगह दी जाती थी. सिखों के बीच विवादों को किसी अदालत के बजाय यहीं सुलझाया जाता था.”
छाओ यान के अनुसार शुरुआत में शंघाई में आ रहे सिख ब्रितानी सरकार के वफ़ादार थे, लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद स्थिति बदली. ख़ासकर कोमागाता मारू घटना के बाद.
साल 1914 में हॉन्ग कॉन्ग से कनाडा पहुंचे जापानी स्टीमशिप कोमागाटा मारू को वैंकुवर में घुसने नहीं दिया गया और उसे वापस भारत लौटा दिया गया था. इस स्टीमशिप में कई सिख भी थे. इससे सिख काफ़ी नाराज़ हुए.
छाओ यान कहते हैं, “सिखों को लगा कि जहां उन्होंने ब्रितानी साम्राज्य के लिए काफ़ी कुछ किया था, उनके साथ गोरे लोगों के मुक़ाबले भेदभाव व्यवहार किया गया. इसलिए वो बहुत नाराज़ हुए और कई लोग सैन-फ़्रांसिस्को में गदर आंदोलन में शामिल हो गए.”
सैनफ्रांसिस्को और पंजाब के बीच सीधा शिपिंग संपर्क नहीं होने के कारण शंघाई आंदोलनकारियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन गया.
गदर आंदोलन का मक़सद था भारत से ब्रितानी शासन को उखाड़ फेंकना.
किताब में एक बुद्धा सिंह का ज़िक्र है जिन्हें यान ने अपनी किताब में शंघाई पुलिस फ़ोर्स में सबसे प्रभावशाली सिख बताया है, लेकिन किताब में उनकी कोई तस्वीर नहीं है. एक सिख रिटायर्ड सिख पुलिस कर्मचारी और क्रांतिकारी ने 6 अप्रैल 1927 की सुबह बुद्धा सिंह की हत्या कर दी.
छाओ यान बताते हैं, “बुद्धा सिंह ब्रितानी सरकार के बहुत वफ़ादार थे. उन्होंने सिख गुरुद्वारों में एजेंट भेजे ताकि विदेश से आए और शंघाई में छिपे सिख क्रांतिकारियों के नेटवर्क का पता लगाया जा सके. वो इन क्रांतिकारियों की पहचान, उनका पता ब्रितानी अधिकारियों को बता देते थे जिससे उनका पता लगाना आसान हो जाता था. बुद्धा सिंह के कारण शंघाई में गदर आंदोलन फ़ेल हो गया.”
1916 और 1949 के बीच दो बातें हुईं. रूस में क्रांति के कारण कई सिखों ने प्रेरणा के लिए रूस का रुख किया. उधर चीनी राष्ट्रवादियों ने ब्रितानी शासकों को बाहर खदेड़ने के लिए सिखों का साथ पकड़ा.
साल 1927 के आसपास शंघाई एक तरह से एसएमसी और ब्रिटेन विरोधी विभिन्न गुटों जैसे गदर पार्टी, चीनी राष्ट्रवादियों आदि के बीच अखाड़ा बन गया था.
साल 1941 में जापान ने चीन पर आक्रमण करके शंघाई पर कब्ज़ा कर लिया जिससे शंघाई पर ब्रितानी असर ख़त्म हो गया.
दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है इसलिए जापानी अधिकारियों ने सिखों का साथ पकड़ा.
छाओ यान कहते हैं, “साल 1943 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूरोप से एशिया पहुंचे और इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) की स्थापना की, उसका पहला हेडक्वॉर्टर सिंगापुर था जो बाद में खिसककर यैंगान चला गया. इस कारण शंघाई आईएएनए का ब्रांच जैसा बन गया. सुभाष चंद्र बोस ख़ुद शंघाई आए और यहां के सिख समुदाय से आईएनए में शामिल होकर ब्रिटेन के खिलाफ़ युद्ध की बात कही. उन्होंने सिखों से वायदा किया कि वो उन्हें वापस भारत लेकर जाएंगे.”
साल 1949 में एक बार फिर शंघाई की स्थिति बदली और शहर पर राष्ट्रवादियों का कब्ज़ा हो गया.
यान बताते हैं, “चीनी राष्ट्रवादी कभी भी भारतीयों या सिखों को पुलिसवालों के तौर पर नौकरी नहीं करने देते. इसलिए सिखों के पास यहां कोई नौकरी नहीं रही और उन्हें शंघाई छोड़कर ऑस्ट्रेलिया, अमरीका और कनाडा जैसे देशों में जाना पड़ा. यही है शंघाई में सिखों की कहानी.”